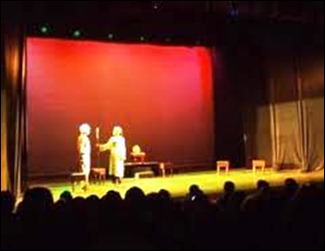नाटक साहित्य
“काव्येषु नाटक रम्यम्”
हमारे देश में नाट्य-लेखन और अभिनय की बहुत लम्बी और समृद्ध परंपरा रही है। संस्कृत नाटकों की परम्परा तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही रही है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने नाटक को सबसे अधिक रमणीय और “पंचमवेद” कहा है। उन्होंने प्रचलित नाट्य लोकपरम्पराओं को नियमबद्ध किया और “नाट्यशास्त्र” की रचना की। उन्होंने नाटक की सम्पूर्ण रचना-प्रक्रिया, सहयोगी कला रूप और रंगमंच पर प्रस्तुति, प्रेक्षागृह के स्वरूप, भेद, आकार आदि पर प्रमाणित सामग्री भी प्रस्तुत की। इसी प्रकार लोकनाटक भी हमारे देश में सदियों से अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ काफ़ी प्रसिद्ध रहा है।
मध्य-युग में आकर प्रेक्षागृहों और नाट्य-प्रदर्शनों का क्रमशः ह्रास होता गया। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति में नटों के प्रति हेय भावना व्यक्त किया गया। इस कारण से रंगकर्मियों और अभिनेताओं की प्रतिष्ठा घटी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भी राजप्रासादों से जुड़ी हुई रंगशालाओं को तहस-नहस कर 
“मध्यकालीन भारत में जिस आतंक और अस्थिरता का साम्राज्य था, उसने यहां की प्राचीन रंगशालाओं को तोड़-फोड़ दिया।”
दुख की बात है कि शास्त्र और लोक की यह सुदृढ़ परम्परा रहते हुए भी नाटक और रंगमंच हमारे जीवन से एकम कटता गया। नाटकों के इस अभाव के बारे में आ. रामचन्द्र शुक्ल का कहना है कि उन दिनों नाटकशालाओं का अभाव था, जबकि ब्रजरत्नदास शान्तिमय वातावरण का अभाव इसका कारण मानते हैं। मध्ययुगीन सामंती पतनशीलता ने रंगमंच के प्रति उदासीनता का भाव पैदा किया। इस काल में जातीय उत्साह के अभाव के अलावा मुसलमान शासकों में इस कला के प्रति प्रोत्साहन का अभाव भी रहा।
डॉ. गुलाब राय के अनुसार गद्य का अभाव भी एक कारण था। कुल मिलाकर उस युग का अनुपयुक्त वातावरण हिन्दी साहित्य के आदिकाल एवं मध्यकाल 
“उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू को छोड़ हिन्दी नाटक खेलने को तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिन्दी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था?”
हालाकि इस पूरे दौर में लोक नाट्य की परंपराएं पहले की तरह गतिमान रहीं। अंग्रेज़ी शासन की स्थापना ने पश्चिम के नाटकों और रंगमंच से हमारा परिचय कराया। इस परिचय से हम प्रेरित हुए और अपनी नाट्य परंपरा की फिर से खोज करने लगे। वर्षों तक पारसी नाटक कम्पनियों के व्यावसायी और सतही मनोरंजक नाट्य प्रदर्शनों का बोलबाला रहा। इसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक और साहित्यिक स्तर के नाटक लिखने की कोशिशें रंगमंच से दूर हटती गईं। नाट्य साहित्य के समीक्षक नाटकों को दो खाने में बांटकर देखने लगे – साहित्यिक नाटक और रंगमंचीय नाटक। व्यावसायिक और रंगमंचीय नाटकों की प्रतिक्रिया में रचनाकार कुछ ऐसा सृजन करने लगे जिसे शुद्ध साहित्यिक नाटक की संज्ञा दी जाए। ऐसे रचनाकार रंगमंच से कटे हुए रहते और नाटक की विधागत मौलिकता और जटिलता का उन्हें ज्ञान ही न होता। ऐसे में सिर्फ़ कल्पना से की गई नाट्य रचना अपना मूल्य स्थापित नहीं कर पाई और नाट्य-लेखन रंगभूमि के जीवित संदर्भ से कट गया।
इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारतेंदु हरिश्चन्द्र का युगांतकारी व्यक्तित्व उभरता है जिन्होंने नाटक प्रस्तुति के माध्यम और कला संबंधी विशेषताओं को अच्छी तरह से समझा और नाट्य साहित्य पर योजनाबद्ध तरीक़े से काम किया।
बाकी़ चर्चा अगले अंक में ... (ज़ारी है)!!
***
संदर्भ ग्रंथ
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास – सं. डॉ. नगेन्द्र, सह सं. डॉ. हरदयाल
२. डॉ. नगेन्द्र ग्रंथावली – खंड ९
३. हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास – हजारीप्रसाद द्विवेदी
४. हिन्दी साहित्य का इतिहास – डॉ. श्यम चन्द्र कपूर
५. हिन्दी साहित्य का इतिहास – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
६. मोहन राकेश, रंग-शिल्प और प्रदर्शन – डॉ. जयदेव तनेजा
७. हिन्दी नाटक : उद्भव और विकास – डॉ. दशरथ ओझा
८. रंग दर्शन – नेमिचन्द्र जैन