भारत में हिंदी का वर्तमान और इंग्लैंड में अंग्रेज़ी का अतीत एक जैसा-अंग्रेज़ों के भाषा प्रेम तथा समर्पणभाव का अनोखा उदाहरण
राइटली एक्सप्रेस्ड के ललित कुमार जी ने अपने एक लेख लिखा है कि "ईमानदारी से कहूँ तो मैं आज तक नहीं समझ पाया कि “हिंदी सेवा” आखिर है क्या चीज़? मैंने कभी “अंग्रेज़ी सेवा” या “फ़्रेंच सेवा” तो नहीं सुना।" उनके उस लेख के बाद मैं बहुत विचलित हुआ कि हिंदी सेवा या हिंदी प्रेम नामक कोई भावना नहीं होती है। इसका मतलब तो यही है कि भारत केवल एक राष्ट्र है जिससे प्रेम करना, राष्ट्रप्रेम, या देशसेवा, देश प्रेम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हिंदी भाषा तो ऐसी चीज़ है जिससे अपना काम तो चला लिया जाए, हिंदी में पुस्तकें लिखकर बेच लिया जाए परंतु उससे कोई लगाव न रखा जाए। इसी प्रकार माँ केवल माँ शब्द है उससे प्रेम करना या उसकी सेवा करने जैसा कुछ भी नहीं है। ललित जी हिंदी भाषी हैं, हिंदी उनकी मातृभाषा है परंतु इससे उनको कोई लगाव नहीं है। यह मात्र संप्रेषण का माध्यम है।
ललित जी का कहना है कि भाषा से प्रेम करने का उदाहरण कहीं नहीं या किसी भाषा के संदर्भ में नहीं मिला। इसलिए ललित जी के उसी विचार के संदर्भ में मैंने उसी अंग्रेज़ी का उदाहरण लेते हुए जिससे हिंदी का संघर्ष है, एक लंबा लेख लिखा है जिसमें हिंदी भाषा की तुलना अंग्रेज़ी भाषा के इतिहास से की गई है। अंग्रेज़ी भाषा के प्रेमियों ने अपने ही देश में अंग्रेज़ी के लिए जो संघर्ष किया क्योंकि उन्हें अपनी भाषा से प्रेम और लगाव था। मैं चाहता हूं कि इस लेख पूरा पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया भी लिखें।
-डॉ. दलसिंगार यादव
सम्भवतः भारत में बहुत थोड़े लोग यह जानते हैं कि जिस प्रकार आज हम विदेशी भाषा अंग्रेज़ी के प्रभाव से आक्रांत होकर स्वदेशी भाषाओं की उपेक्षा कर रहे हैं उसी प्रकार किसी समय इंग्लैंड भी विदेशी भाषा फ़्रेंच के प्रभाव से इतना अभिभूत था कि न केवल सारा सरकारी कामकाज फ़्रेंच भाषा में होता था बल्कि उच्च वर्ग के लोग अंग्रेज़ी में बात करना भी अपनी शान के खिलाफ़ समझते थे। किंतु आगे चलकर फ़्रेंच के स्थान पर अंग्रेज़ी लागू की गई तो उसका भारी विरोध हुआ और उसके विषय में सारे वे ही तर्क दिए गए जो आज हमारे यहाँ हिंदी के विरोध में दिए जा रहे हैं। फिर भी कुछ राष्ट्रभाषा प्रेमी अंग्रेज़ों ने विभिन्न प्रकार के उपायों से किस प्रकार अंग्रेज़ी का मार्ग प्रशस्त किया इसकी कहानी न केवल अपने आप में रोचक है बल्कि हमारी आज की हिंदी विरोधी स्थिति के निराकरण के लिए भी उपयुक्त्त मार्ग सुझा सकती है।
इंग्लैंड में अंग्रेज़ी का पराभव क्यों?
वैसे अंग्रेज़ी इंग्लैंड की अत्यंत प्राचीन भाषा रही है। यहाँ तक कि जब इस देश का नाम ₹इंग्लैंड₹ के रूप में विख्यात नहीं हुआ था तब भी इंग्लैंड भाषा का अस्तित्व था। वस्तुतः इंग्लिश नाम इंग्लैंड के आधार पर नहीं पड़ा, इंग्लिश भाषा के प्रचलन के कारण ही इस भूभाग को इंग्लैंड की संज्ञा प्राप्त हुई तथा दसवीं शताब्दी तक यह समूचे राष्ट्र को बहुमान्य भाषा के रूप में प्रचलित थी। परंतु ग्यारहवीं में सदी के उत्तरार्ध में एकाएक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण इंग्लैंड में ही अंग्रेज़ी का सूर्य अस्त होने लगा। बात यह हुई कि नार्मंस लोगों का इंग्लैंड पर आधिपत्य हो गया। उनका नायक ड्यूक ऑफ़ विलियम इंग्लैंड के तत्कालीन शासक हेराल्ड को युद्ध में पराजित करके स्वयं सिंहासनारूढ़ हो गया और तभी से इंग्लैंड पर फ़्रेंच भाषा एवं फ़्रांसीसी संस्कृत के प्रभाव की अभिवृद्धि होने लगी क्योंकि स्वयं नार्मंस की भाषा और संस्कृति पूर्णतः फ़्रेंच थी।
जब शासक वर्ग की भाषा फ़्रेंच हो गई तो स्वभावतः न केवल सारा राजकाज फ़्रेंच में होने लगा बल्कि शिक्षा, धर्म और समाज ने भी अंग्रेज़ी के स्थान पर फ़्रेंच प्रतिष्ठित होने लगी। उच्च वर्ग के जो लोग सरकारी पदों के अभिलाषी थे या जो शासक वर्ग से मेल-जोल बढ़ा कर अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहते थे वे बड़ी तेज़ी से फ़्रेंच सीखने लगे तथा कुछ ही वर्षों में यह स्थिति आई कि धनिकों, सामंतों शिक्षकों, पादरियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों आदि सबने फ़्रेंच को ही अपना लिया और अंग्रेज़ी केवल निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों, किसानों और मजदूरों की भाषा रह गई। अपने आपको शिक्षक कहने या कहलवाने वाले लोग केवल फ़्रेंच का ही प्रयोग करने लगे और अंग्रेज़ी जानते हुए भी अंग्रेज़ी बोलना अपनी शान के खिलाफ़ समझने लगे। दूसरी बात यह कि कभी-कभी उन्हें अपने अनपढ़ नौकरों या मज़दूरों से बात करते समय अंग्रेज़ी जैसी हेय भाषा में भी बोलने को विवश होना पड़ता था। आगे चलकर इंग्लैंड नार्मंस के आधिपत्य से तो मुक्त हो गया किंतु उनकी भाषा के प्रभाव से फिर भी मुक्त्त नहीं हो पाया। इसका कारण यह था कि जिन अंग्रेज़ी राजाओं का इंग्लैंड में शासन था वे स्वयं अपने फ़्रेंच के प्रभाव से अभिभूत थे। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ का ननिहाल फ़्रांस में था तो कुछ की ससुराल पेरिस में थी। अनेक राजकुमारों और सामंतों ने बड़े यत्न से पेरिस में रह कर फ़्रेंच भाषा सीखी थी जिसे बोलकर वे अपने आपको उन लोगों की तुलना में श्रेष्ठ समझते थे जो बेचारे केवल अंग्रेज़ी ही बोल सकते थे। दूसरे, उस समय फ़्रेंच भाषा और संस्कृति सारे यूरोप में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। फिर अंग्रेज़ी की तुलना में फ़्रेंच का साहित्य इतना समृद्ध था कि उसे विश्व ज्ञान की खिड़की ही नहीं दरवाज़ा कहा जाता था। ऐसी स्थिति में भले ही इंग्लैंड स्वतंत्र हो गया हो पर वहाँ अंग्रेज़ी की प्रतिष्ठा कैसे संभव थी?
इंग्लैंड में फ़्रेंच भाषा के आधिपत्य को बनाए रखने में कुछ राजाओं ने व्यक्तिगत कारणों से भी बड़ा योगदान दिया। उदाहरण के लिए हेनरी तृतीय (1216-1272) का विवाह फ़्रांस की राज कुमारी से हुआ था जो अपने साथ भारी दान दहेज़ के अलावा अपने साथ मामाओं, सैकड़ों रिश्तेदारों और उनके सेवकों की पलटन भी लेकर आई थी जिन्हें उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करना हेनरी के लिए आवश्यक था। भला ऐसा न करके वह अपनी नव विवाहिता दुल्हन का मन कैसे दुखा सकता था? इसका परिणाम यह हुआ कि एक बार पुनः सभी सरकारी महकमों एवं कार्यालयों पर फ़्रेंच का पूरी तरह अधिकार हो गया। जो लोग फ़्रेंच बोल सकते थे, लिख सकते थे या उस भाषा में लिखवा सकते थे उन्हीं की सरकार में सुनवाई हो सकती थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ी पढ़ना पढ़ाना बेकार था। इसलिए सामान्य पाठशालाओं में भी अंग्रेज़ी की अपेक्षा फ़्रेंच की ही अधिक पढ़ाई होती थी। किंतु 14वीं सदी में इन स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई तथा धीरे-धीरे अंग्रेज़ी का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके कई कारण थे, एक तो यह की 1337 से 1453 तक इंग्लैंड और फ़्रांस के बीच युद्ध चला जिसे इतिहासकारों ने शतवर्षीय युद्ध की संज्ञा दी है। इस युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों में फ़्रेंच भाषा और फ़्रेंच संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनपने लगी।
अंग्रेज़ी का पुनः अभ्युदय
अब फ़्रेंच को शत्रु जाति की भाषा के रूप में देखा जाने लगा। दूसरे, इसी शताब्दी में निम्नवर्ग एवं मध्यम वर्ग में नवजागरण की लहर आई। ये लोग अपने स्वत्व एवं अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। 1381 में मज़दूरों ने अधिक वेतन के लिए आंदोलन किया जिसके फ़लस्वरूप उनकी स्थिति में सुधार हुआ। देश के विभिन्न संगठनों ने अपनी अन्य माँगों के साथ-साथ अपनी स्वभाषा अंग्रेज़ी को भी मान्यता देने की माँग की। दूसरी ओर, मध्य वर्ग के लोग भी लोग भी जो अपने बच्चों को पेरिस नहीं भेज पाते थे तथा गाँव के स्कूलों में ही पढ़ा कर संतुष्ट हो जाते थे अंग्रेज़ी के समर्थक बन गए। उच्च वर्ग में भी अब शुद्ध फ़्रेंच बोलने वाले बहुत कम रह गए थे। सही बात तो यह है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ लंदन रिटर्न लोग अंग्रेज़ी के बड़े-बड़े प्रॉफ़ेसरों पर भी अपने अंग्रेज़ी ज्ञान एवं उच्चारण की धाक जमाते रहे हैं, वैसे ही लंदन ने कुछ पेरिस रिटर्न लोगों की धाक थी। पेरिसनुमा फ़्रेंच बोलने वाले अपने ही देश इंग्लैंड के उन लोंगों की खिल्ली उड़ाते थे जो स्थानीय विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़कर टूटी-फूटी या अशुद्ध फ़्रेंच बोलते थे।
धीरे-धीरे अंग्रेज़ी के पक्ष में लोकमत जागृत हुआ और 1362 में पार्लियामेंट में एक अधिनियम "स्टेच्यूट ऑफ़ प्लीडिंग" (अधिवक्त्ताओं का अधिनियम) पारित हुआ जिससे इंग्लैंड के न्यायालयों में अंग्रेज़ी का प्रवेश संभव हो गया। हालाँकि इस अधिनियम का भी उस समय के बड़े-बड़े अधिवक्त्ताओं ने भारी विरोध किया क्योंकि अंग्रेज़ी में न्याय और कानून संबंधी पुस्तकों का सर्वथा अभाव था। फिर भी तर्क दिया गया कि ऐसी स्थिति में कैसे बहस की जा सकेगी और कैसे न्याय सुनाया जाएगा? एक देशी भाषा के लिए न्याय की हत्या की जा रही है। स्थति यह थी कि वैधानिक दृष्टि से भले ही अंग्रेज़ी को मान्यता मिल गई परंतु कचहरियों का अधिकांश कार्य काफ़ी समय फ़्रेंच भाषा में ही चलता रहा।
चौदहवीं शती में न्यायालयों के अतिरिक्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी अंग्रेज़ी का पठन-पाठन प्रचलित हुआ। ऑक्सफ़ोर्ड के कुछ अध्यापकों ने भी लैटिन के अतिरिक्त अंग्रेज़ी की शिक्षा देने की व्यवस्था की।
अंग्रेज़ी लिखना ग़ुनाह - अतः अंग्रेज़ी में सृजन कार्य के लिए क्षमा याचना
यद्यपि इस प्रकार इंग्लैंड के जन साधारण में अंग्रेज़ी का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा था फिर भी उच्च वर्ग के विद्वानों एवं विद्वत्ता की भाषा वह अभी तक नहीं बन पाई थी। फ़्रेंच का प्रभुत्व थोड़ा कम हुआ तो उसका स्थान लैटिन और ग्रीक ने ले लिया। पंद्रहवीं शती के पुनर्जागरण युग में ये शास्त्रीय भाषाएं समस्त यूरोप में ज्ञान-विज्ञान की भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थीं। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ी में लिखने वाले लोग प्रायः हेय दृष्टि से देखे जाते थे। इसका प्रमाण इसी युग की अनेक रचनाओं की भूमिका से मिलता है जहां उसके रचयिता ने अंग्रेज़ी में लिखने के लिए अपनी सफ़ाई दी है। उदाहरण के लिए ज्यादा 14वीं शती के आरंभ में ही एक अंग्रेज़ी पुस्तक के रचयिता ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "भले ही भाषा की दर से मैं हीन समझा जाऊं फिर भी मेरे मन में जो कुछ है उसे अवश्य बता देना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर अंग्रेज़ी में लिखा जाए तो उसी सब लोग समझ सकते हैं। सही बात तो यह है कि उन क्लर्कों को (सरकारी कर्मचारियों) की अपेक्षा जो फ़्रेंच जानते हैं उस बेचारे जनसाधारण को दिव्य ज्ञान की अधिक आवश्यकता है जो केवल अंग्रेज़ी ही जानते हैं। अतः मैं सोचता हूँ कि यदि अंग्रेज़ी में कोई अच्छी चीज लिखी जाए तो यह एक पुण्य का कार्य होगा।"
इसी प्रकार एश्कम नामक लेखक ने अपनी पुस्तक "टांक्सो पिलस" की भूमिका में स्पष्ट किया है कि उसके लिए ग्रीक या लैटिन में लिखना अधिक आसान था फिर भी उसने सर्व साधारण के हित को ध्यान में रखकर ही अंग्रेज़ी में लिखने का दुस्साहस किया है। पर इससे भी महत्वपूर्ण वक्तव्य 16वीं शती के एक अन्य लेखक की इलिएट का है। इसमें अपनी चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक कलस ऑफ़ हेल्थ अर्थात् "स्वास्थ्य का कवच" की भूमिका में अंग्रेज़ी में लिखने के लिए क्षमा याचना करते हुए लिखा है – "यदि चिकित्सक लोग मुझ पर इसलिए कुपित हैं कि मैंने अंग्रेज़ी में क्यों लिखा तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर ग्रीक लोग ग्रीक में लिखते हैं, रोमन लोग स्वभाषा लैटिन में लिखते हैं तो फिर यदि हम लोग अपनी भाषा अंग्रेज़ी में लिखे तो इसमें क्या बुराई है?"
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किस प्रकार पंद्रहवीं से सोलहवीं शती में अंग्रेज़ी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें लिखना विद्वानों की दृष्टि से हेय समझा जाता था तथा जो ऐसा करने का प्रयास करते थे वे अपनी सफाई में कोई न कोई तर्क देने को विवश होते थे। इसकी तुलना हमारे मध्य कालीन में हिंदी के आचार्य केशव दास की मनःस्थिति से भी की जा सकती है जिन्होंने अपनी एक रचना में लिखा था - हाय जिस कुल के दास भी भाषा (हिंदी) बोलना नहीं जानते अर्थात ये भी संस्कृत में बोलते हैं उसी कुल में मेरे जैसा मतिमंद कवि हुआ जो भाषा (हिंदी) में काव्य-रचना करता है। वस्तुतः जब कोई राष्ट्र विदेशी संस्कृति एवं भाषा से आक्रांत हो जाता है तो उस स्थिति में स्वदेशी भाषा एवं संस्कृति के उन नायकों में आत्मलघुता या हीनता की भावना का आ जाना स्वाभाविक है।
प्रेयसियों के प्रेम पत्रों की दुहाई
यद्यपि सोलहवीं शती में अनेक विद्वान अंग्रेज़ी को अपनाने लगे थे फिर भी अंग्रेज़ी और विदेशी भाषाओं का विवाद शांत नहीं हुआ था। अब भी उच्च वर्ग में ऐसे अनेक लोग थे जो युक्तियों व तर्कों से इंग्लैंड में फ़्रेंच का वर्चस्व बनाए रखने के हिमायती थे, जैसे जॉन बटन ने फ़्रेंच को प्रचलित रखने के पक्ष में तीन तर्क दिए थे। उनके अनुसार, एक तो न केवल अपने देश में बल्कि आसपास के पड़ोसी राज्यों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए फ़्रेंच आवश्यक है। दूसरे, ज्ञान विज्ञान और कानून की सारी पुस्तकें फ़्रेंच में ही हैं। तीसरे, इंग्लैंड की सभी सुशिक्षित महिलाएँ एवं भद्रजन अपने प्रेम पत्रों का आदान-प्रदान फ़्रेंच में ही करते हैं। यह तीसरा तर्क सचमुच रोचक है जो कुछ लोगों को हास्यास्पद प्रतीत हो सकता है किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं जब कि वर्ग विशेष की रुचि या अनुकंपा के कारण कोई भाषा अपना अस्तित्व बनाए रखती है। उदाहरण के लिए पंजाब में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पूर्व पुरुषों की भाषा प्रायः उर्दू थी जबकि महिलाओं की शिक्षा दीक्षा हिंदी में होती थी। इसलिए कहा जाता है कि पुरुष वर्ग को हिंदी केवल इसलिए पढ़नी पड़ती थी कि वे अपनी पत्नियों तथा माताओं/बहनों के साथ पत्राचार कर सकें। इसलिए पंजाब में हिंदी की परंपरा जीवित रखने का श्रेय वहां की महिलाओं को जाता है।
ख़ैर, इन परिस्थितियों के होते हुए भी राष्ट्रभाषा-प्रेमी अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं हारी। वे स्वीकार करते थे कि फ़्रेंच, लैटिन और ग्रीक की तुलना में अंग्रेज़ी भाषा और उसका साहित्य नगण्य है, तुच्छ है। फिर अंततः वह उनकी अपनी भाषा है। ये दूसरों की माताएँ अधिक सुंदर और संपन्न हों तो क्या हम अपनी मां को केवल इसलिए ठुकरा देंगे कि वह उनकी तुलना में असुंदर और अकिंचन है। कुछ ऐसी ही भाषा में अंग्रेज़ी भाषा के कट्टर समर्थक रिचर्ड मुलकास्टर ने 1582 में लिखा -
"आई लव रोम, बट लंडन बेटर, आई फ़ेवर इटली, बट इंग्लैंड मोर, आई ऑनर लैटिन, बट आई वर्शिप द इंग्लिश।"
अर्थात्, मैं रोम को प्यार करता हूँ पर लंदन को उससे भी अधिक, मैं लैटिन का समर्थक हूं पर इंग्लैंड का उससे भी अधिक समर्थन करता हूँ और मैं लैटिन का सम्मान करता हूँ पर अंग्रेज़ी की पूजा करता हूं। क्या हमें हिंदी के बारे में ऐसी ही धारणा नहीं रखनी चाहिए?
कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज़ी के समर्थकों ने अपने आंदोलन को तर्क और विवाद के बल पर नहीं बल्कि भावना के बल पर सफ़ल बनाया। उन्होंने अपने देशवासियों के मस्तिष्क को नहीं उनके हृदय को झकझोरकर उनके स्वाभिमान और राष्ट्र-प्रेम को उद्वेलित किया। इसी का परिणाम था कि इस सदी के अंत तक उच्च वर्ग का भी दृष्टिकोण अंग्रेज़ी के प्रति पर्याप्त अनुकूल हो गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि एक ओर तो रिचर्ड जैसे विद्वान ने 1595 में अंग्रेज़ी भाषा की उच्चता पर लेख लिख कर उसका ज़ोरदार समर्थन किया तो दूसरी ओर, सर फ़िलिप सिडनी जैसे विद्वान ने घोषित किया कि यदि भाषा का लक्ष्य अपने हृदय और मस्तिष्क की कोमल कल्पनाओं को सुन्दर एवं मधुर शब्दावली में व्यक्त करना है तो निश्चय ही अंग्रेज़ी भाषा भी इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा से उतनी ही सक्षम है जितनी की विश्व की अन्य भाषाएँ।
सत्रहवीं शती के आरंभ तक इंग्लैण्ड में अंग्रेज़ी के विरोध का वातावरण तो शांत हो गया तथा आम धारणा बन गई कि स्वदेशी भाषा को हर कीमत पर अपनाना है किंतु जब इसे एक व्यावहारिक रूप दिया जाने लगा तो सबसे बड़ी कठिनाई शब्दावली की आई। अंग्रेज़ी को समृद्ध करने के लिए ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ कैसे लिखे जा सकते थे जबकि तद्विषयक शब्दावली का उसमें सर्वथा अभाव था। ज्ञान विज्ञान की बात तो दूर, उस समय शब्द संपदा की दृष्टि से अंग्रेज़ी इतनी दरिद्र थी कि प्रशासन, कला, समाज, धर्म और दैनिक जीवन से संबंधित सामान्यत शब्द भी उसके पास अपने नहीं थे, फ़्रेंच या अन्य भाषाओं से उधार लिए हुए थे। उदाहरण के लिए, प्रशासनिक शब्दावली में अंग्रेज़ी के पास अपने केवल दो शब्द थे- किंग (राजा) और क्वीन (रानी)। शेष सारे शब्द फ़्रेंच भाषा से आयातित थे – गवर्नमेंट, क्राउन, स्टेट, एंपायर, रॉयल, कोर्ट, काउंसिल, पार्लियामेंट, असेंबली, स्टैच्यूट, वार्डन, मेयर, प्रिंस, प्रिंसेस,ड्यूक, मिनिस्टर, मैडम आदि। इसी प्रकार न्यायालय और कानून संबंधी सारी शब्दावली भी प्रायः फ़्रेंच से आयातित है, जैसे, जस्टिस, क्राइम, वार, ऐडवोकेट, जज, प्ली, सूट, पेटीशन, कॉम्प्लेंट, समन,एविडेंस, प्रूफ़, प्लीडेड, प्रॉपर्टी, एस्टेट। ये शब्द भी अंग्रेज़ी के अपने नहीं हैं। फिर कला और साहित्य संबंधी अधिकांश शब्द अंग्रेज़ी के पास नहीं थे। अतः आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, ब्यूटी, कलर, फ़िगर, इमेज, ऐप्रोच, रोमांस, स्टोरी, ट्रैजडी, प्रिफ़ेस, टाइटिल, चैप्टर, पेपर जैसे शब्द भी फ़्रेंच से लेने पड़े। इतना ही नहीं एक इतिहासकार ने तो यहां तक कहा है कि फ़्रेंच शब्दावली के अभाव में कोई भी अंग्रेज़ अपने रहन-सहन से लेकर खान-पान तक की भी कोई क्रिया संपन्न नहीं कर सकता था क्योंकि उसे ड्रेस, फसल, गारमेंट, कॉलर, पेटीकोट, बूट, बटन, ब्लू, ब्राउन, डिनर, सुपर, टेस्ट, फ़िश, बीफ़, मटन, टोस्ट, स्किट, क्रीम, शूगर, ग्रेप, ऑरेंज, लेमन, चेरी जैसे शब्दों के लिए भी फ़्रेंच पर निर्भर करना पड़ता है। "ए हिस्टरी ऑफ़ द इंग्लिश लैंग्वेज" के लेखक अलबर्ट सी. बॉफ़ के अनुसार लगभग दस हजार से ज़्यादा शब्द तो अकेले फ़्रेंच से ही अंग्रेज़ी में अपनाया लिए गए थे परंतु आगे चलकर विश्व की अन्य भाषाओं से भी हजारों शब्द ग्रहण किए गए। उनके मतानुसार यह कहना अत्युक्त्ति न होगी कि अंग्रेज़ी में इस समय लगभग पचास से भी अधिक भाषाओं से हजारों शब्द ग्रहण किए जा चुके थे जिनमें अधिकांश फ़्रेंच-लैटिन-ग्रीक-इटैलियन और स्पैनिश से थे।
हिंदी की भाँति अंग्रेज़ी भाषा के विरुद्ध क्लिष्टता का शोर मचा था
जब अंग्रेज़ी में विभिन्न भाषाओं से बड़ी संख्या में ऐसे शब्दों को स्वीकार किया गया जो पहले से अंग्रेज़ी में प्रचलित नहीं थे तो यह स्वाभाविक था कि जन सामान्य के लिए वह अत्यंत दुर्बोध एवं क्लिष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त विदेशी शब्दों के अधिक मिश्रण से स्वभाषा की शुद्धता का भी प्रश्न उपस्थित हुआ। अतः विद्वानों के एक वर्ग ने शुद्धता एवं क्लिष्टता के दृष्टिकोण से विदेशी शब्दों के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा। किंतु इसके प्रत्युत्तर में अनेक विद्वानों ने कठिन शब्दों के शब्दकोश तैयार करके क्लिष्टता की समस्या को हल करने की चेष्टा की। इस प्रकार के प्रयासों में एन. वैलो की "यूनिवर्सल एटिमॉलॉजिकल इंग्लिश डिक्शनरी" (1719), राबर्ट काडरो का "द अल्फ़ाबेटिकल टेबल ऑफ़ हाई वर्ड्स" तथा एडवर्ड फ़िलिप की "न्यूवर्ड ऑफ़ वर्ड्स" जैसी कृतियां उल्लेखनीय हैं। क्या उन लोगों के कार्य अपनी भाषा की सेवा नहीं हैं?
जहां तक भाषा की शुद्धता की बात है, अधिकांश लेखकों और साहित्यकारों ने भी इस संबंध में उदार दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विदेशी शब्दों को ग्रहण किए जाने का समर्थन किया। हिंदी के समर्थकों की भी यही राय है।
आगे चल कर स्वदेशी एवं विदेशी शब्दों का झगड़ा सदा के लिए तब समाप्त हो गया था जब 1755 में डॉक्टर जॉनसन द्वारा प्रकाशित अंग्रेज़ी के प्रथम प्रामाणिक शब्दकोश "ए डिक्शनरी ऑफ़ इंग्लिश लैंग्वेज" में उन सारे शब्दों को समेट लिया गया जो अंग्रेज़ी में प्रयुक्त हो सकते थे भले ही वे मूल अंग्रेज़ी के हों या विदेशी भाषाओं से आयातित। इस प्रकार इन शब्दों पर अंग्रेज़ी का लेबल लगाकर उसे एक अत्यंत सम्पन्न भाषा का रूप दे दिया गया। यह दूसरी बात है कि जॉनसन के विरोधी अब भी बराबर कहते रहे कि उनके शब्दकोश में पंद्रह प्रतिशत शब्दों को छोड़कर शेष सारे विदेशी हैं। पर इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जब भाषा की अभिव्यंजना शक्ति की समस्या हल हो गई तो उसमें ज्ञान विज्ञान के साहित्य की रचना के मार्ग में खड़े सारे अवरोध स्वतः दूर हो गए। अंग्रेज़ जाति ने अपने राष्ट्रभाषा प्रेम की प्रगाढ़ का परिचय देते हुए विदेशी भाषाओं की खिड़कियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान पर निर्भर न रहकर स्वभाषा के द्वार सबके लिए खोल दिए। इससे सभी देशों की सभी वर्गों के लिए ज्ञान का आवागमन उपयुक्त्त रूप से होने लगा और साथ ही इससे स्वभाषा के उन सहस्रों लोगों को भी रोज़गार मिला जो विभिन्न भाषाओं के ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों और उनके मूल विचारों अथवा उनका अविकल अनुवाद अंग्रेज़ी में प्रस्तुत करने में सक्षम थे। वस्तुतः अंग्रेज़ी भाषा के अभ्युदय का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई जाति सच्ची राष्ट्रीयता का सुदृढ़ संकल्प एवं पूरी शक्ति से जुट जाए तो वह किस प्रकार सर्वथा गंवारू, अपरिष्कृत, दरिद्र एवं अधम कही जाने वाली भाषा को भी एक दिन विश्व की श्रेष्ठ भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सकती है।
हिंदी की इस स्थिति से तुलना
यदि अंग्रेज़ी भाषा की प्रतिष्ठा के इस संघर्षपूर्ण इतिहास से हिंदी की स्थिति की तुलना करें तो दोनों में अनेक समानताएँ दृष्टि गोचर होती हैं – (1) यद्यपि दोनों ही अपने-अपने देश की अत्यंत बहुप्रचलित भाषाएं थीं फिर भी विदेशी भाषा भाषी लोगों के प्रशासन काल में दोनों का ही पराभव होना आरंभ हुआ और वे शीघ्र ही अपने गौरवपूर्ण पद से वंचित हो गईं तथा उनका स्थान शासक वर्ग की विदेशी भाषा ने ले लिया। (2) शासक वर्ग की विदेशी भाषा को अपनाने में उच्च वर्ग के धनिकों, सामंतों एवं शिक्षितों ने बड़ी तत्परता का परिचय दिया। (3) विदेशी भाषा के प्रभाव से दोनों ही देशों (इंग्लैंड और भारत) के लोग इतने अभिभूत हो गए कि वे स्वदेशी भाषा को अत्यंत ही हेय एवं उपेक्षा योग्य मानते हुए उसमें बात करना भी अपनी शान के खिलाफ़ समझने लगे। (4) विदेशी शासकों के प्रति विद्रोह की भावना एवं स्वभाषा के प्रति अनुराग की प्रेरणा से ही अंग्रेज़ी और हिंदी के पुनः अभ्युत्थान की प्रक्रिया आरंभ हुई।(5) दोनों ही देशों में पार्लियामेंट द्वारा स्वदेशी भाषाओं को मान्यता मिल जाने के बाद भी उनका व्यावहारिक प्रयोग बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ा। (6) विदेशी भाषा के समर्थक एक ओर तो अभिव्यंजना शक्त्ति और साहित्यिक समृद्धि का गीत गाते रहे, तो दूसरी ओर स्वदेशी भाषा की हीनता और दरिद्रता का ढिंढोरा पीटते रहे तथा (7) जब स्वदेशी भाषा को समृद्ध करने के लिए नए शब्दों का प्रचलन किया जाने लगा तो उसके विरोधी उसपर क्लिष्टता और दुर्बोधता का आरोप लगाने लगे।
इस प्रकार अंग्रेज़ी और हिंदी के पराभव एवं पुनरुत्थान की कहानी परस्पर बहुत मिलती-जुलती है। परंतु दोनों में थोड़ा अंतर भी है जिसके कारण हिंदी की प्रगति में आज तक बाधाएं उपस्थित हो रही हैं। एक, अँग्रेज़ जाति में राष्ट्रीयता की भावना जितनी दृढ़ और गंभीर है, उतनी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तो हममें रही किंतु उसके बाद वह बिखरती चली गई। सम्भवतः इसका प्रमुख कारण यह है कि हमने अपने संविधान को अमरीका की नकल पर ढालने के लिए भारत के उप प्रदेशों और प्रान्तों को भी राज्यों की संज्ञा देकर यह भ्रम उत्पन्न कर दिया मानो भारत एक सुगठित देश न होकर अनेक राज्यों का समूह या संघ है। इससे निश्चय ही क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। इसके कारण हिंदी का विरोध केवल अंग्रेज़ी के हिमायतियों द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य प्रान्तीय या क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थकों द्वारा भी होने लगा जबकि हिंदी की प्रतिद्वंद्विता अंग्रेज़ी से है न कि भारत की अन्य भाषाओं से। ऐसी स्थिति में हम हिंदीतर क्षेत्रों में न सही, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही जो राजस्थान से लेकर बिहार तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, पूरी तरह हिंदी लागू कर दें तो यह भी कम महत्व की बात नहीं होगी। किंतु स्वयं हिंदी भाषा भाषी वर्ग में भी अभी अब अंग्रेज़ी के प्रति मोह बना हुआ है। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि न केवल केंद्र में, बल्कि हिंदी भाषा भाषी राज्यों में भी सरकारी अधिकारियों और उच्च प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं तथा ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक अंग्रेज़ी का ही प्रचलन है। अतः जो अंग्रेज़ी की उपेक्षा करते हैं कि वे अपने भविष्य के निर्माण की दृष्टि से घाटे में रहते हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में जनसाधारण में अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने का फ़ैशन और भी ज़ोरों से फैला है।
दूसरे, अंग्रेज़ी के समर्थकों ने अपनी भाषा की शब्द संपदा और अभिव्यंजना शक्त्ति में वृद्धि करने के लिए विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं के बहुप्रचलित शब्दों को उन्मुक्त्त भाव से अपनाया, भले ही कट्टरवादियों की दृष्टि में इसमें एक ऐसी अशुद्ध भाषा बन गई जिसमें अधिकांश शब्द विदेशी हैं। परंतु इससे अंग्रेज़ी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों की रचना और अनुवाद के कार्य में तेज़ी से प्रगति हुई। इसकी तुलना में हम पहले कृत्रिम ढंग से विदेशी शब्दालियों तथा पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द गढ़ने के बखेड़े में पड़ गए जो कभी भी समाप्त न होने वाली स्थिति है क्योंकि जब तक हम पचास वर्ष में आज की प्रचलित शब्दावली का अनुवाद करेंगे तब तक उतने ही नए शब्द सामने आ जाएँगे। विज्ञान की जिस गति से प्रगति हो रही है उसे देखते हुए यह स्वाभाविक है। फिर इस प्रकार कृत्रिम ढंग से बनी हुई शब्दावली को प्रचलित करना और प्रयोग में लाना अब भी अपने आप में टेढ़ी खीर है। पिछला अनुभव हमें बता रहा है कि ऐसे नव निर्मित शब्दों के अधिकांश शब्दकोश केवल सरकारी अलमारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वे वास्तविक प्रयोग में बहुत कम आ रहे हैं। अतः इससे अच्छा यह है कि हम ज्ञान विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को ज्यों का त्यों अपना लें और यदि उसके साथ-साथ सहज रूप में अपनी शब्दावली भी विकसित होती हो तो उसे भी अपनाते रहें। पर यदि हम अपनी नई शब्दावली की ही प्रतीक्षा करते रहेंगे तो सम्भवतः यह कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। उस स्थिति में यही कहना पड़ेगा कि न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी।
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा हिंदी की उपेक्षा और अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार
देश में वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग योजना आयोग के माध्यम से प्रधान मंत्री के सीधे प्रभार में रखा गया था। इस आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। इसके सदस्य थे, डॉ. अशोक गांगुली, रिज़र्व बैंक के बोर्ड में निदेशक और कई प्राइवेट कंपनियों के बोर्डों में सदस्य हैं, डॉ. जयति घोष, जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं, डॉ. दीपक नैयर, जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं , डॉ. पी. बलराम, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के निदेशक हैं, डॉ. नंदन निलेकनी, कंप्यूटर विज्ञानी हैं, डॉ. शुजाता रामदोई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ंडामेंटल रिसर्च में गणित के प्रोऱेसर हैं, डॉ. अमिताभ मट्टू, जम्मू विश्व विद्यालय के उप कुलपति हैं। इनमें से कोई भी हिंदी का समर्थक नहीं है, हालांकि हिंदी बोल सकते हैं। मैंने पित्रोदा जी को हिंदी बोलते सुना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत कर दी है और उसके कार्यान्वयन का काम शुरू हो गया है।
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य ज्ञान के क्षेत्र में देश को 21 वीं शताब्दी में सबसे आगे ले जाने के लिए शिक्षा और अनुसंधान हेतु आधारभूत और मज़बूत ढांचा तैयार करना है। आयोग ने अपनी सिफ़रिश में कहा है कि देश में अंग्रेज़ी की पढ़ाई पहली कक्षा से शुरू की जाए और दो भाषाएं, अर्थात, अंग्रेज़ी तथा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए। आयोग ने हिंदी की सिफ़ारिश नहीं की है और न कि त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात की है। प्नधान मंत्री ने भी इसे स्वीकार कर ली है और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफ़रिशों को लागू कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी है। क्या भारत के सभी स्कूलों में अंग्रेज़ी की स्तरीय पढ़ाई शुरू हो जाएगी और सभी विद्यार्थी फ़र्राटे से अंग्रेज़ी बोलने लग जाएंगे या उन्हीं लोगों को आगे आने का अवसर देने की सुनियोजित चाल है जो धनाढ्य, संपन्न और शहर में रहकर शिक्षा पाने में सक्षम हैं?
त्रिभाषा सूत्र ही सरलतम हल
देश की भाषा समस्या जनता जनित नहीं है बल्कि यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जनित है। जन प्रतिनिधियों ने ही इसे 1947 में ही स्वीकार कर लिया था कि देश में एक संपर्क भाषा हो और वह भारत की ही भाषा हो कोई विदेशी भाषा न हो। संविधान लागू होने के बाद पंद्रह साल का समय भाषा परिवर्तन के लिए रखा गया था और वह समय केवल केंद्र सरकार की भाषा के लिए ही नहीं बल्कि भारत संघ के सभी राज्यों के लिए भी रखा गया था कि उस दौरान सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अपनी राजभाषा निर्धारित कर लेंगी एवं उन्हें ऐसी सशक्त बना लेंगी कि उनके माध्यम से समस्त सरकरी काम काज किए जाएंगे तथा राज्य में स्थित शिक्षा संस्थाएं उनके माध्यम से ही शिक्षा देंगी। यह निर्णय 1949 में ही किया गया था राज्यों ने अपनी-अपनी राजभाषा नीति घोषित कर दी थी। यद्यपि वहां भी पूरी मुस्तैदी से काम नहीं हुआ क्योंकि राज्यों के सामने शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण अन्य आवश्यक समस्याएं थीं जिनपर अविलंब ध्यान देना था। उस चक्कर में राज्य सरकारों ने राजभाषाओं की समस्या को टाल दिया था परंतु किसी भी सरकार ने अंग्रेज़ी को राजभाषा के रूप में अनंत काल तक बनाए रखने की मंशा नहीं व्यक्त की। अतः राज्यों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी राजभाषाओं को प्रचलित करने के लिए अपने यहां भाषा विभागों की स्थापना की और कार्यालयी भाषा की शिक्षा देना प्रारंभ किया, भाषा प्रयोग की समीक्षा करने लगे तथा प्रशासनिक शब्दावली बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। राज्य सरकारों ने उसी निर्धारित समय में अपनी भाषाओं को संवर्धित किया और आज नागालैंड के सिवाय सभी राज्यों ने अपनी राज्य भाषाओं में काम करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में यह और भी आवश्यक हो गया है कि देश में राज्यों के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया जाए।
अनेक समितियां और आयोग बने परंतु किसी ने भी हिंदी के प्रश्न को समय सीमा से परे रखने की सिफ़ारिश नहीं की है। राजभाषा आयोग, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सभी ने हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में ही शिक्षा दीक्षा देने की सिफ़ारिश की है। तब संविधान में हिंदी को अनिश्चित काल के लिए टालने की बात कहां से आई? यह निश्चित रूप से कोई सोची समझी चाल तथा प्रच्छन्न विद्वेष की भावना लगती है। इसे समझने और ग्रासरूट स्तर पर चेतना जागृत करने की आवश्यकता है।
हिंदी को वास्तविक रूप में कामकाज की भाषा बनाना हो तो देश में त्रिभाषा सूत्र सच्चे मन से तथा कड़ाई से लागू करना होगा। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की कठिनाइयों पर शिक्षा आयोग (1964-66) ने विस्तार से विचार किया है। व्यावहारिक रूप से त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की कठिनाइयों में मुख्य है स्कूल पाठ्यक्रम में भाषा में भारी बोझ का सामान्य विरोध, हिंदी क्षेत्रों में अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए अभिप्रेरण (मोटिवेशन) का अभाव, कुछ हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी के अध्ययन का विरोध तथा पांच से छह साल तक, कक्षा छठी से दसवीं तक दूसरी और तीसरी भाषा के लिए होने वाला भारी खर्च और प्रयत्न। शिक्षा आयोग ने कार्यान्वयन की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा है कि गलत योजना बनाने और आधे दिल से सूत्र को कार्यान्वित करने से स्थिति और बिगड़ गई है। अब वह समय आ गया है कि सारी स्थिति पर पुनर्विचार कर स्कूल स्तर पर भाषाओं के अध्ययन के संबंध में नई नीति निर्धारित की जाए। अंग्रज़ी को अनिश्चित काल तक, भारत की सहचरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण यह बात और भी आवश्यक हो गई है।
आस्था और भाषा के प्रति निष्ठा
अतः ऐसी परिस्थिति में कार्यालयों में हिंदी को प्रचलित करने तथा स्टाफ़ सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए सतत और सत्यनिष्ठा के साथ शिक्षण प्रशिक्षण का हर संभव प्रयास करना होगा एवं हिंदी की सेवा से जुड़े हर व्यक्ति को अपने अहम् को दूर रखकर प्रयास करना होगा। गुरु रवींद्र नाथ टैगोर की चार पंक्तियां उल्लेखनीय हैं –
सांध्य रवि बोला कि लेगा काम अब यह कौन,
सुन निरुत्तर छबि लिखित सा रह गया जग मौन,
मृत्तिका दीप बोला तब झुकाकर माथ,
शक्ति मुझमें है जहां तक मैं करूंगा नाथ।।
हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के मुताबिक प्रयास करना होगा। ऐसे में हम यह चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप से यह प्रश्न करे कि यह बड़ा और दुष्कर कार्य कैसे होगा और उसका उत्तर भी स्वयं ढूंढे, कुछ इस प्रकार –
बड़ा काम कैसे होता है, पूछा मेरे मन ने,
बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदुवाणी,
किंतु अहम् छोटा हो जिससे सहज मिलें सहयोगी,
दोष हमारा श्रेय राम का, यह प्रवृत्ति कल्याणी।।
फ़र्क़ शब्दावलियों के अपनाने का
इंग्लैंड में अंग्रेज़ी लागू करने में नई शब्दावली की प्रतीक्षा नहीं की गई। ज्ञान विज्ञान के सारे साहित्य को अनूदित किए बिना ही शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी को लागू कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ इस स्वतः ही विश्व का सारा ज्ञान विज्ञान रूपांतरित होकर मौलिक रूप में अंग्रेज़ी में अवतरित हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब प्रकाशकों ने देखा कि शिक्षा का माध्यम अब अंग्रेज़ी हो गया है तो उन्होंने रातों-रात भाग दौड़ करके उन लेखकों को पकड़ा जो अपने ज्ञान विज्ञान को विदेशी भाषा में व्यक्त कर सकते। व्यापारियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण हर विषय की एक से एक अच्छी पुस्तक बाजार में आने लगी। सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। परंतु हिंदी में हम इसके विपरीत चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि पहले सारा ज्ञान विज्ञान हिंदी में आ जाए फिर उसे शिक्षा का माध्यम बनाएं। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेज़ी में होती रहेगी तब तक क्यों कोई लेखक हिंदी में पुस्तक लिखेगा और क्यों कोई प्रकाशक उसे छापेगा? और यदि उसे छाप भी लिया तो कोई उससे क्यों खरीदेगा? केवल सरकार ही ऐसा कर सकती है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। अपनी अकादमियों के माध्यम से सरकार के इस प्रकार के प्रयास का परिणाम यह हुआ कि आज प्रत्येक राज्य को हिंदी अकादमियों के भंडारों में ऐसी पुस्तकों से भरे पड़े हैं जो बिना विशेष रुचि या परिश्रम के, पारिश्रमिक की लालच में हिंदी में अनूदित एवं प्रकाशित हैं। माँग तो तब हो जब उसके अनुकूल परिस्थितियां पैदा हों। अतः पहले हिंदी को शिक्षा एवं शासन के माध्यम के रूप में लागू किया जाए तो फिर तद्विषयक हिंदी पुस्तकों की माँग स्वतः ही उत्पन्न होगी। किंतु हम इसके विपरीत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहले तैरना सीख लें फिर पानी में उतरें जबकि वास्तविकता का क्रम इस से उल्टा है।
इसी तरह एक वर्ग ऐसा है जो अंग्रेज़ी की खिड़की पर मुग्ध होकर अपनी भाषा के द्वार को बंद किए हुए है। वह यह नहीं समझता है कि खिड़की आख़िर खिड़की ही है। वह द्वार का स्थान कभी नहीं ले सकती। जब तक हम स्वभाषा के ज्ञान के द्वार का उपयोग खुलकर नहीं करेंगे तब तक विश्व ज्ञान के अबाध आदान प्रदान के लिए हमें एक खिड़की पर ही निर्भर करना पड़ेगा।
ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास है कि अंग्रेज़ी के अभ्युत्थान की प्रक्रिया से हम कोई सबक ले सकें तो वह हमारी राजभाषा की प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है और हमारी तद्विषयक अनेक समस्याओं के समाधान का उपाय सुझा सकता है।
-डॉ. दलसिंगार यादव
*******

![IMG_0130_thumb[1] IMG_0130_thumb[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGFpO73xngpmzYKvtlasW7TngYv6eUFbX3YO2JEqeGUlAmzh7udrwl8vdjV8dhfsO1jDa4bDX_Qmh5FCmNxiRKZOf9b7SQjbdn6EhN_3daEH7rHdLQw86iO3HTqIagKQC9jbFyPSuqcKai/?imgmax=800) मनोज कुमार
मनोज कुमार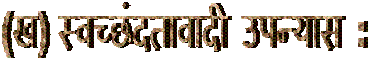



![[19012010014[4].jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV71RlwivX0bUmXCNZlqQALyZln-UzRaedL1Ot77dVkhJMevY2l8QErSz86vQUUoSvgcdramQHSRPnnLOaXoDcN1zGjNgG-Jfzm0NKf942YCDZeJWQI1S16_FyRPMFwazpw6P71I0V9z92/s1600/19012010014%5B4%5D.jpg) डॉ. रमेश मोहन झा
डॉ. रमेश मोहन झा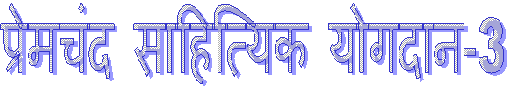
![[IMG_0568[4].jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlHXaYFLYJaIpICkSREplnYJ6gZ0ickEbXUqhPd4ansk5kmEcvg4sHXcDpBivqojy_9r66P7FM0afq7juq7Xp7LY03jl7jZgVDqcHpu4T8Hw0CYhVVazAA7Jst38wPEsS86qJyjOPJvIs/s1600/IMG_0568%5B4%5D.jpg)





