 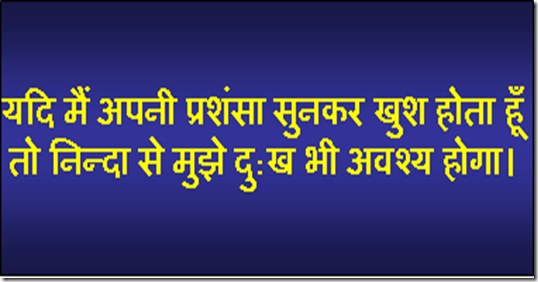 |
काव्य प्रयोजन (भाग-3)पाश्चात्य विद्वानों के विचार |
| पिछले दो पोस्टों मे हमने काव्य-सृजन का उद्देश्य और संस्कृत के आचार्यों के विचार की चर्चा की थी। संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, यही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है। आइए अब इसी विषय पर पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा उसकी चर्चा करें।
यूनानी दार्शनिक प्लेटो का काल ई.पू. 427-347 का है। यह समय एथेन्स के पतन का था। इस समय आध्यात्मिक और नैतिक ह्रास में काफ़ी बढोत्तरी हुई। अतः उनकी चिन्ता थी कि कैसे आदर्श राज्य की स्थापना हो और चरित्र निर्माण द्वारा नैतिक मूल्यों की रक्षा कैसे हो? उन्होंने भी लोकमंगल, अर्थात् सत्य और शिव, के आधार पर काव्य के प्रयोजन को देखा। प्लेटो का मानना था कि काव्य का उद्देश्य मानव-प्रकृति में जो महान और शुभ है, नैतिक और न्यायपरायण है, उसका उसका उद्घाटन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने कला के आनंद सिद्धांत से आगे बढकर लोकमंगल सिद्धांत को महत्वपूर्ण बतया।
पाश्चात्य विद्वानों मे जिन्होंने काव्य प्रयोजन पर चर्चा की एक और महत्वपूर्ण नाम है लांजाइनस का। इन्होंने अपने ग्रंथ ‘परिइप्सुस’ में कहा है कि काव्य वाणी का ऐसा वैशिष्ट्य है, चरमोत्कर्ष है, जिससे महान कवियों को जीवन में प्रतिष्ठा और यश मिलता है। कारण यह है कि उसका सृजन, पाठक को मात्र जागृत करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके मन में अह्लाद उत्पन्न करने में सक्षम होता है। उनका मानना था कि महान सृजन महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लांजाइनस ने काव्य में उदात्त-तत्व की बात की थी। उदात्त की शक्ति से पाठक कृति-प्रभाव को ‘आत्मातिक्रमण’ के रूप में ग्रहण करता है। इसमें भी भाव-परिष्कार, भाव-उन्नयन या विरेचन सिद्धांत शामिल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया। महान काव्य वही है जो सभी को सब कालों मे आनंद प्रदान करे और समय जिसे पुराना न कर सके। इस प्रकार ‘आनंद’ या ‘आत्मातिक्रमण’ ही साहित्य का मुख्य प्रयोजन है। |
मंगलवार, 31 अगस्त 2010
काव्य प्रयोजन (भाग-3) पाश्चात्य विद्वानों के विचार
गुरुवार, 29 जुलाई 2010
काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है :: काव्य लक्षण-13 (पाश्चात्य काव्यशास्त्र-1)
काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है::काव्य लक्षण-13 (पाश्चात्य काव्यशास्त्र-1) |
|
प्लेटो की विवेचना में अनुकरण का अनुकरण है। इस तरह यह सत्य से दूर हो जाता है। अरस्तु ने भी काव्य की परिभाषा नहीं की, किन्तु जो विचार व्यक्त किए उसके आधार पर काव्य लक्षण का निर्धारण किया जा सकता है।
प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। उन्होंने अपने ही गुरु के विचारों का तर्कों के आधार पर खंडन किया। उन्हें लगा कि प्लेटो की विवेचना में अनुकरण का अनुकरण है। इस तरह यह सत्य से दूर हो जाता है। अरस्तु ने भी काव्य की परिभाषा नहीं की, किन्तु जो विचार व्यक्त किए उसके आधार पर काव्य लक्षण का निर्धारण किया जा सकता है।
इस प्रकार अरस्तु के अनुसार काव्य लक्षण का निर्धारण इस प्रकार होता है, “काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है।”डॉ. नगेन्द्र का भी यही मानना था कि काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। आधुनिक शब्दावली में अगर कहें तो “काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा जीवन का पुनःसृजन है।”(चित्र : आभार गूगल खोज) |