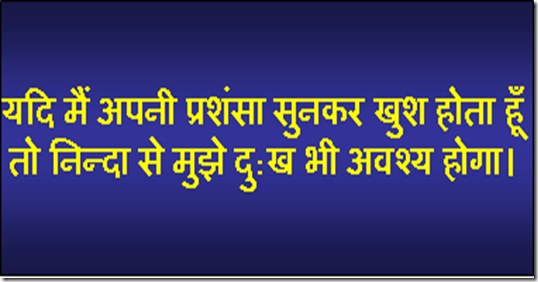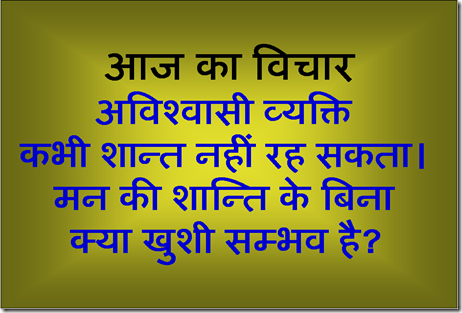काव्य प्रयोजन
आधुनिक काल
मनोज कुमार
आदिकाल और मध्यकाल
पूरा भक्तिकाव्य यह धारना व्यक्त करता है कि
“मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी”
अर्थात् प्रेम ही जीवन को दिव्य बनाता है। बैर नहीं। प्रेम से ही बैकुंठ की प्राप्ति संभव है।
भक्ति-रस में डूब कर ही लोग महान बन सकते हैं। भक्तिशास्त्र में कहा गया,
“प्रेमा पुमर्थो महान”।
भक्ति काल के साहित्य में यह भाव पुरुषार्थ के रूप में प्रखर रूप से आया। सूफ़ी कवियों ने भी इसे प्रतिस्थापित किया।
निर्गुणपंथी संत कबीरदास ने अंधविश्वास, कुरीतियों और रूढ़िवादिता का विरोध किया। विषमताग्रस्त समाज में जागृति पैदा कर लोगों को भक्ति का नया मार्ग दिखाना इनका उद्देश्य था। जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। उन्होंने हिंदु-मुस्लिम एकता के प्रयास किए। उन्होंने राम और रहीम के एकत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने दोनों धर्मों की कट्टरता पर समान रूप से फटकार लगाई।
 वहीं ‘पद्मावत’ के रचयिता जायसी ने सता शक्ति के अभिमान पर प्रहार किया।
वहीं ‘पद्मावत’ के रचयिता जायसी ने सता शक्ति के अभिमान पर प्रहार किया।
‘रमचरितमानस’ में संत तुलसी दास ने कहा है
“कीरति भनितिभूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कह हित होई॥”
अर्थात् कीर्ति-प्रीति-भनिति का एक ही उद्देश्य है - ‘लोकमंगल की भावना’।
इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भक्ति-काव्य का प्रयोजन था लोकमंगल की भावना।
रीतिकाव्य में दरबारी काव्य के मूल्यों का पोषण हुआ। कहा गया,
“सरस राग-रीति-रंग”
इसी धारणा में पूरी तरह डूब जाना उस काल के सामंतों की नियति थी। इस काल में शृंगारिकता, रसिकता और झूठी शास्त्रीयता को कवि लोग पकड़े रहे।
“राधिका कान्ह सुमिरन को बहाने”
कविता का मुख्य प्रयोजन बन गया भोग, केलि-क्रीड़ा, विलास-पूर्ण मनोरंजन। उनका तो लक्ष्य था
तजि तीरथ हरि-राधिका तन दुति कर अनुराग।
जेहि ब्रज केलि निकुंज मग पग-पग होतु प्रयाग॥
नायिका के शरीर से अनुराग करो – यही पूरे रीतिकाल का जीवन दर्शन था। इस काल में शृंगार-रस को रसराज का रूप मिला। यह एक प्रकार से कलाकाल है। इस काल के अधिकांश कवि, बिहारी, देव, मतिराम, घनानंद, आदि रसवाद के पोषक हैं। ये कवि प्रेमी नहीं, रसिक हैं।
नवजागरण काल
इतिहास में एक काल आया पुनर्जागरण का। यह काल सांस्कृतिक नवजागरण का काल है। इस समय में ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था तक सीमित हो गई। हमारी इस धारणा में बदलाव नवजागरण की मानसिकता से आया। सांस्कृतिक नवजागरण की प्रक्रिया का उद्भव दो जातीय सांस्कृतियों के टकराने से हुआ। भारत में अंग्रेज़ी हुक़ूमत आ चुकी था। इसका विरोध भी हो रहा था।
सहित्य का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं था। भारतेंदु हरिश्चद्र ने ‘कविवचन सुधा’ में स्वदेशी वस्तुओं को व्यवहार में लाने का प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित किया। यह प्रतिज्ञा-पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है।
नवजागरण की चेतना बंगाल में आरंभ हुई। फिर यह हिन्दी प्रदेशों में पहुंची। शनैः-शनैः यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक रूप धारण करती गई। इस युग के लगभग सभी लेखकों ने अंग्रेज़ों के दमन चक्र का अपने-अपने लेखन में विरोध किया।
विरोध का सर्वाधिक समर्थ माध्यम था नाटक। नटकों ही नहीं सभी तरह की सृजन-ध्वनि में साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध स्पष्ट था। इसके अलावा अपसी कलह और वैमनष्व को भी समाप्त करने की चेतना जगाने का इस काल के साहित्य का प्रयोजन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस काल की सृजनात्मक ध्वनि थी सामाजिक धार्मिक सुधार चेतना।
1857 की जन क्रांति विफल हो गई तो इसका दर्द भी रचनाओं में स्पष्ट रूप से आया तथा साथ ही लोकजागरण की चेतना का विकास इस काल के काव्य का प्रयोजन हो गया।
1857 की जन क्रांति के बाद स्वाधीनता संग्राम में प्रसार हुआ। जनता में जागृति आई। सभी तबके के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि नवजागरण की चेतना का उद्भव और विकास अंग्रेज़ों की देन नहीं बल्कि हमारी चिंतन परंपरा की ऊर्जा का उग्र विस्फोट है। उस काल की रचनाओं में आंतरिक राष्ट्र ध्वनि कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं,
“सरबस लिए जात अंग्रेज़”, … “धन विदेश चलि जात” … या “भारतवासी रोए”।
इस प्रकार हम पाते हैं कि नवजागरण काल के काव्य की अंतः ध्वनि अंग्रेज़ी साम्राज्यवादी लूटतंत्र के प्रति विरोध, विक्षोभ, विद्रोह और बग़ावत को व्यक्त करना था।