बुधवार, 3 नवंबर 2010
कविताओं में बिंब और उनसे जुड़ी हुई संवेदना
बुधवार, 6 अक्टूबर 2010
काव्य प्रयोजन (भाग-११) मनोविश्लेषणवादी चिंतन
| काव्य प्रयोजन (भाग-११) मनोविश्लेषणवादी चिंतन |
| पिछली दस पोस्टों मे हमने (१) काव्य-सृजन का उद्देश्य, (लिंक) (२) संस्कृत के आचार्यों के विचार (लिंक), (३)पाश्चात्य विद्वानों के विचार (लिंक), (४) नवजागरणकाल और काव्य प्रयोजन (५) नव अभिजात्यवाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) (६) स्वच्छंदतावाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) (७) कला कला के लिए (८) कला जीवन के लिए (लिंक) (९) मूल्य सिद्धांत अय्र (१०) मार्क्सवादी चिंतन की चर्चा की थी। जहां एक ओर संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, ही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया। नवजागरणकाल के साहित्य का प्रयोजन था मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। जबकि नव अभिजात्यवादियों का यह मानना था कि साहित्य प्रयोजन में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। स्वछंदतावादी मानते थे कि कविता हमें आनंद प्रदान करती है। कलावादी का मानना था कि कलात्मक सौंदर्य, स्वाभाविक या प्राकृतिक सौंदर्य से श्रेष्ठ होता है। कला जीवन के लिए है मानने वालोका मत था कि कविता में नैतिक विचारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मूल्य सिद्धांत के अनुसार काव्य का चरम मूल्य है – कलात्मक परितोष और भाव परिष्कार। मार्कसवादियों के अनुसार साहित्य जनता के लिए हो। इसका प्रयोजन तो मानव-कल्याण है। आइए अब पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा को आगे बढाएं। |
|
अरस्तू के विरेचन सिद्धांत या भाव-परिष्कार को मनोविश्लेषणशास्त्र के अंतर्गत उठाया गया। इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना था कि काव्य, काम-वासना के रेचन या उदात्तीकरण का माद्ध्यम है। मनोविश्लेषण शास्त्रियों ने काव्य प्रयोजन को परिभाषित करते हुए कहा, “मानव की भावनाओं का उन्नयन-परिष्करण और उदात्तीकरण करना ही काव्य का प्रयोजन है।” अर्थात् मन के भीतर उत्पन्न हुए विकृतियों से मुक्ति दिलाना और चित्त का शमन ही काव्य का उद्देश्य है। इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना था कि सौंदर्य परक काव्य और उद्दाम शृंगार परक क्कव्य-नाटक-उपन्यास के अध्ययन से मनव के मन की काम-भावना परिष्कृत होती है। इसका शमन होता है। एडलर भी मनोविश्लेषणशास्त्री थे। उनका कहना था कि साहित्य ‘ग्रंथियों’ से मुक्ति दिलाने का माध्यम है। जीवन की जटिलता को अनुभूति की आंच में सहजता से पकाकर पाठक को परोस देना भी साहित्य का एक प्रयोजन कहा जा सकता है।
इस प्रकार मनोविश्लेषणवादी चिंतन में हम पाते हैं कि काव्य का कम है भावों या विचारों का रेचन या परिष्कार करना। |
| पश्चिम में काव्य प्रयोजन संबंधी अनेक विचारधाराओं का प्रतिपादन हुआ। पर अगर गौर से देखें तो हम पाते हैं कि कुल मिलाकर दो समूह थे, एक आनंदवादी और दूसरा कल्याणकारी। इन दोनों के भीतर काव्य सृजन का प्रयोजन मानव चेतना का विस्तार है। सृजन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। रचनाकार इस प्रक्रिया को आगे बढाता है। भावों और विचारों को सम्प्रेषित करता है। इस प्रकार जीवन की जटिलता को अनुभूति की आंच में सहजता से पकाकर पाठक को परोस देना भी साहित्य का एक प्रयोजन कहा जा सकता है। पर कुल मिलाकर अगर देखा जए तो काव्य का प्रयोजन है भावों और विचारों का सम्प्रेषण तथा सांस्कृतिक चेतना का विस्तार और परिष्कार। |
बुधवार, 29 सितंबर 2010
काव्य प्रयोजन (भाग-१०) मार्क्सवादी चिंतन
काव्य प्रयोजन (भाग-१०)मार्क्सवादी चिंतन |
| पिछली नौ पोस्टों मे हमने (१) काव्य-सृजन का उद्देश्य, (लिंक) (२) संस्कृत के आचार्यों के विचार (लिंक), (३)पाश्चात्य विद्वानों के विचार (लिंक), (४) नवजागरणकाल और काव्य प्रयोजन (५) नव अभिजात्यवाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) (६) स्वच्छंदतावाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) (७) कला कला के लिए (८) कला जीवन के लिए (लिंक) और (९) मूल्य सिद्धांत की चर्चा की थी। जहां एक ओर संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, ही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया। नवजागरणकाल के साहित्य का प्रयोजन था मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। जबकि नव अभिजात्यवादियों का यह मानना था कि साहित्य प्रयोजन में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। स्वछंदतावादी मानते थे कि कविता हमें आनंद प्रदान करती है। कलावादी का मानना था कि कलात्मक सौंदर्य, स्वाभाविक या प्राकृतिक सौंदर्य से श्रेष्ठ होता है। कला जीवन के लिए है मानने वालोका मत था कि कविता में नैतिक विचारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मूल्य सिद्धांत के अनुसार काव्य का चरम मूल्य है – कलात्मक परितोष और भाव परिष्कार। आइए अब पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा को आगे बढाएं। |
| मार्क्स ने जिस मूल्य-सिद्धांत की बात की थी, मार्क्सवादी उसके आधार पर साहित्य की विचारधारा, शिल्प और मूल्य-चेतना पर विचार करते हैं। अधिकांश विद्वान जो इस विचारधारा के समर्थक हैं वे साहित्य का अध्ययन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों की सहायता से करते हैं। इस सिद्धांत के अनुयाईयों का मानना है कि सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों मे आर्थिक व्यवस्था, वर्ग-संघर्ष का विशेष हाथ होता है। वे यह मानते हैं कि साहित्य रूप या सृजन की साहित्यिक पृष्ठभूमि का अध्ययन, दोनों को आर्थिक-सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर ही समझा ज सकता है। मार्क्सवाद साहित्य को भी समाज के परिवर्तन के एक टूल के रूप में मानता है। उनका मानना है कि लोगों में जागरण साहित्य के द्वारा पैदा किया जा सकता है। वे पूंजीवादी और सामंतवादी साहित्य का विरोध करते हैं। मार्क्सवाद ने ‘कला कला के लिए सिद्धांत’ में जो व्यक्तिवाद-भाववाद की चर्चा की गई है, उसका विरोध किया। साहित्य का उद्देश्य परिभाषित करते हुए मार्क्सवादियों का कहना है कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को प्रबुद्ध सामाजिकता की दृष्टि से सम्पन्न करना होना चाहिए। साथ ही यह अनीति और अनैतिकता के ख़िलाफ़ जागरूकता पैदा करे। मनुष्य अर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन जीता है। साहित्य उसके पूरे जीवन से जुड़ा है। साहित्य के द्वारा मनुष्य की ऐसी भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणिमात्र से जोड़ती हैं। इसलिए साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। मनुष्य का इंद्रिय-बोध, भावनाएं और आंतरिक प्रेरणाएं भी साहित्य से व्यंजित होती हैं। और साहित्य का यह पक्ष स्थायी होता है। मार्क्सवाद विचारधारा के समर्थक यह कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य कृति की मूल्य-व्यवस्था पर ध्यान देना है। क्योंकि संघर्षपरक, समाज-सापेक्ष, लोकमंगलकारी मूल्य मानव-समाज को आगे बढाते हैं। इस सिद्धांत के मानने वालों के अनुसार आनंदवादी, रीतिवादी मूल्य मानव को विकृत करते हैं। साहित्य का वास्तविक प्रयोजन तो जीवन-यथार्थ का वास्तविक उद्घाटन है। काडवेल से लेकर जार्ज लूकाच तक सभी मार्क्सवादी चिंतक काव्य का प्रयोजन मानव-कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति मानते रहे हैं। किसी भी रचना के मूल्य और मूल्यांकन में ही उसका प्रयोजन निहित रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवाद चिंतन में कलावादी मूल्यों से अधिक मानववादी, मनवतावादी, नैतिक उपयोगितावादी या यूं कहें कि सामाजिक मूल्यों का अधिक महत्व दिया गया है। उनके अनुसार साहित्य जनता के लिए हो। इसका प्रयोजन तो मानव-कल्याण है। |
गुरुवार, 9 सितंबर 2010
काव्य प्रयोजन (भाग-७) कला कला के लिए
काव्य प्रयोजन (भाग-७)कला कला के लिए |
| पिछली छह पोस्टों मे हमने (१) काव्य-सृजन का उद्देश्य, (लिंक) (२) संस्कृत के आचार्यों के विचार (लिंक), (३) पाश्चात्य विद्वानों के विचार (लिंक), (४) नवजागरणकाल और काव्य प्रयोजन (५) नव अभिजात्यवाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) और (६) स्वच्छंदतावाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) की चर्चा की थी। जहां एक ओर संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, ही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया।। नवजागरणकाल के साहित्य का प्रयोजन था मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। जबकि नव अभिजात्यवादियों का यह मानना था कि साहित्य प्रयोजन में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। स्वछंदतावादी मानते थे कि कविता हमें आनंद प्रदान करती है। आइए अब पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा को आगे बढाएं। |
| उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक में “कला कला के लिए” सिद्धांन्त सामने आया। कुछ हद तक स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति ही कलावाद का रूप धारण कर सामने आई। इस सिद्धांत को फ्रांस के विक्टर कूजे ने प्रतिपादित किया था। बाद में आस्कर वाइल्ड, ए.सी. ब्रैडले, ए.सी. स्विनबर्न, एडगर ऐलन पो, वाल्टर पेटर आदि कलाकारों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांतकारों का मानना था कि काव्यकला की दुनिया स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, अर्थात् जो किसी दूसरे के शासन या नियंत्रण में नहीं हो, बल्कि जिस पर अपना ही अधिकार हो। उनका यह भी मानना था कि कला का उद्देश्य धार्मिक या नैतिक नहीं है, बल्कि ख़ुद की पूर्णता की तलाश है। अपने इन विचारों को रखते हुए कलावादियों ने कहा कि कला या काव्यकला को किसी उपयोगितावाद, नैतिकतावाद, सौन्दर्यवाद आदि की कसौटी पर कसना उचित नहीं है। कलावादियों के अनुसार कला को अगर किसी कसौटी पर परखना ही है तो उसकी कसौटी होनी चाहिए सौंदर्य-चेतना की तृप्ति। उनके अनुसार कला सौंदर्यानुभूति का वाहक है और उसका अपना लक्ष्य आप ही है। कलावाद एक आंदोलन था। उन्नीसवीं शताब्दी में काव्य और कला की हालत दयनीय थी। इसी हालात की प्रतिक्रिया की उपज था यह आन्दोलन। इस आंदोलन के वाहकों का कहना था कि काव्य और कला की अपनी एक अलग सता है। इसका प्रयोजन आनंद की सृष्टि है। “POETRY FOR POETRY SAKE!” अर्थात् अनुभव की स्वतंत्र सत्ता। “This experience is an end in itself, is worth having on its own account, has an intrisic value.” अर्थात् काव्य से प्राप्त आनंद की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इस प्रकार स्वच्छंदतावाद, सौंदर्यवाद और कलावाद तीन अलग-अलग वैचारिक दृष्टिकोण थे। कलावादी का मानना था कि कलात्मक सौंदर्य, स्वाभाविक या प्राकृतिक सौंदर्य से श्रेष्ठ होता है। वाद्लेयर, रेम्बू, मलामें में यह झलक मिलती है। बिम्बवाद तथा प्रतीकवाद कलावाद के ही विस्तार थे। बाद में बाल्ज़ाक और गाटियार आदि ने रूप-विधान पर बल दिया। धीरे-धीरे “कला कला के लिए” सिद्धांत का विकास हुआ और रूपवाद के अलावा संरचनावाद, नयी समीक्षा, नव-संरचनावाद या उत्तर-संरचनावाद, विनिर्मितिवाद आया। |
शनिवार, 4 सितंबर 2010
काव्य प्रयोजन (भाग-6) स्वच्छंदतावाद और काव्य प्रयोजन
काव्य प्रयोजन (भाग-6)
स्वच्छंदतावाद और काव्य प्रयोजन
पिछली पांच पोस्टों मे हमने (१) काव्य-सृजन का उद्देश्य, (लिंक) (२) संस्कृत के आचार्यों के विचार (लिंक), (३) पाश्चात्य विद्वानों के विचार (लिंक), (४) नवजागरणकाल और काव्य प्रयोजन (लिंक) और नव अभिजात्यवाद और काव्य प्रयोजन (लिंक) की चर्चा की थी। जहां एक ओर संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, ही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया।। नवजागरणकाल के साहित्य का प्रयोजन था मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। जबकि नव अभिजात्यवादियों का यह मानना था कि साहित्य प्रयोजन में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। आइए अब पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा को आगे बढाएं।
सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी में विकसित नव अभिजात्यवाद की विचारधारा के साथ-साथ नव-मानववाद का भी विकास हुआ। इस विचारधार में मानव को विश्व के केंद्र में माना गया। इसके अलावा आत्मवाद की भी अवधारण सामने आई। रचनाकार आत्माभिव्यक्ति के लिए अभिप्रेरित हुए।
इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी ........ औद्योगिक क्रांति। इससे सामंतवादी ढांचे का पतन हुआ था और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। इस तरह से प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति की नींव तैयार हो चुकी थी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य स्वर था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यही तीन स्वर उस समय के साहित्य सृजन के प्रयोजन बनकर उभरे।
इस प्रकार काव्य प्रयोजन ने एक नया आयाम ग्रहण किया। नव अभिजात्यवादी तो नियम और संयम में रूढि़बद्ध थे। पर इस काल में इसका भी विरोध हुआ और स्वच्छंदतावाद का उदय हुआ। विलियम ब्लेक (1757-1827) सैम्युअल कॉलरिज (1772-1834) विलियम वर्डसवर्थ (177-1850 ), शैले, कीट्स, बायरन आदि कवि ने इस विद्रोही स्वर को आवाज दी। इनके अनुसर काव्य सृजन का प्रयोजन था,
“आत्म साक्षात्कार, आत्म सृजन और आत्माभिव्यक्ति।”
इस तरह स्वच्छंदतावादियों ने अपने काव्य सृजन का प्रमुख उद्देश्य मानव की मुक्ति की कामना को माना। जहां इनके पूर्ववर्ती नव अभिजात्चादी नियम, संयम संतुलन, तर्क को तरजीह दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्वच्छंदतावादी प्रकृति, स्वच्छंदता, मुक्त-अभिव्यक्ति, कल्पना और भावावेग को अपने सृजन में प्रधानता दे रहे थे।
जीवन में आनंद इनके सृजन का उद्देश्य था। आनंद के साथ साथ रहस्य, अद्भुत और वैचित्र्य में उनकी रूचि थी। स्वच्छंदतावादी मानते थे कि सृजन में सुंदर के साथ अद्भुत का संयोग होना चाहिए। यही उनके काव्य का प्राण तत्व था।
कॉलरिज और वर्डसवर्थ ने काव्य में कल्पना शक्ति पर बल दिया। वर्डसवर्थ ने ‘लिरिकल बैलेड्स’ में कहा,
“कविता हमें आनंद प्रदान करती है।”
इस प्रकार हम पाते हैं कि पश्चिम का स्वच्छंदतावाद भारतीय काव्यशास्त्र के रस-सिद्धांत के बहुत करीब है। हिंदी के आधुनिक आलोचकों में से एक डॉ. नगेन्द्र ने भी माना है कि स्वच्छंदतावाद का आनंदवाद से घनिष्ठ संबंध है।
इस काल के प्रमुख रचनाकारों, शैले, वर्डसवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, बायरन की रचनाओं में आनंद का स्वर प्रमुखता से दिखाई पड़ता है।
स्वछंदतावादी काव्य समीक्षक डा. नगेंद्र ने ‘रस सिद्धांत’ में कहा भी है कि शैले का मानवता की मुक्ति में अटूट विश्वास, वर्डसवर्थ का सर्वात्मवाद, कॉलरिज का आत्मवाद, कीट्स का सौंदर्य के प्रति उल्लासपूर्ण आस्था और बायरन का जीवन के प्रति अबाध उत्साह, आनंदवाद के ही रूप हैं।
शुक्रवार, 3 सितंबर 2010
काव्य प्रयोजन (भाग-5) नव अभिजात्यवाद
काव्य प्रयोजन (भाग-5)नव अभिजात्यवाद और काव्य प्रयोजन |
| पिछली चार पोस्टों मे हमने (१) काव्य-सृजन का उद्देश्य, (लिंक) (२) संस्कृत के आचार्यों के विचार (लिंक), (३) पाश्चात्य विद्वानों के विचार (लिंक) और (४) नवजागरणकाल और काव्य प्रयोजन (लिंक) की चर्चा की थी। जहां एक ओर संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, ही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया।। नवजागरणकाल के साहित्य का प्रयोजन था मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। आइए अब पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा को आगे बढाएं। हमने नवजागरण युग की चर्चा करते हुए पाया कि एक नई चेतना का उदय हुआ। इटली में शुरू हुए इस विचार का धीरे-धीरे फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड तक विस्तार हुआ। पुनरूद्धार और प्रत्यावर्तन के इस यूरोपीय रेनेसां, व्यक्ति को मध्ययुगीन बंधनों से मुक्त करने का यह आंदोलन, व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना को आगे बढ़ाने का प्रबल केंद्र बना। पर बीतते समय के साथ व्यक्ति स्वातंत्र्य की भावना अतिवाद में बदल गई। इससे अराजकता फैलने लगी। इसके कारण लोगों का झुकाव अभिजात्यवाद की ओर होने लगा। नवअभिजात्यवाद के उदय ने साहित्य जगत को भी प्रभावित किया। फ्रांस में अरस्तु के सिद्धांत की नई व्याख्याएं हुई। कार्लीन, रासीन, बुअलो आदि ने नए नियम बनाए। उनका मानना था कि श्रेष्ठ कृतियां वही कही जा सकती हैं जिनमें कथा तथा संरचना की गरिमा हो। वे भव्यता के साथ साथ संतुलन को भी सृजन का प्रमुख गुण मानते थे। अठारहवीं शताब्दी तक यह नियोक्लासिज़्म इंग्लैंड भी पहुंच गया। यहां पर नव अभिजात्य विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता थे डॉ. सैम्युअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन। नव अभिजात्यवादियों का यह मानना था कि साहित्य प्रयोजन में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। |
बुधवार, 1 सितंबर 2010
काव्य प्रयोजन (भाग-4) नवजागरणकाल की दृष्टि
काव्य प्रयोजन (4)नवजागरणकाल और काव्य प्रयोजन |
| पिछली तीन पोस्टों मे हमने (१) काव्य-सृजन का उद्देश्य, (लिंक)(२) संस्कृत के आचार्यों के विचार (लिंक) और (३) पाश्चात्य विद्वानों के विचार (लिंक) की चर्चा की थी। जहां एक ओर संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, ही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया।। आइए अब पाश्चात्य विद्वानों की चर्चा को आगे बढाएं। प्लॉटिनस ने दर्शन के आधार पर विवेचना करते हुए कहा कि कविता उस परम चैतन्य तक पहुंचने का सोपान है। उनके अनुसार कविता के प्रयोजन आनंद और परम चेतना के सौंदर्य का साक्षात्कार है।
नवजागरणकाल में प्राचीन यूनानी-रोमन ज्ञान का पुनरुद्धार हुआ। विज्ञान और तर्क की कसौटी पर वर्तमान की तलाश-परख की गई और रूढ और जर्जर मूल्यों-परम्पराओं का बहिष्कार हुआ। परलोकवाद की जगह इहलौकिक चिंतन को महत्व दिया जाने ल्लगा। धर्मनिरपेक्ष चिंतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। स्पेंसर, मार्लो और शेक्सपियर सरीखे रचनाकारों का सृजन इसी ऊर्जा से ओत-प्रोत है। इस काल के साहित्य का प्रयोजन था मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। |
मंगलवार, 31 अगस्त 2010
काव्य प्रयोजन (भाग-3) पाश्चात्य विद्वानों के विचार
 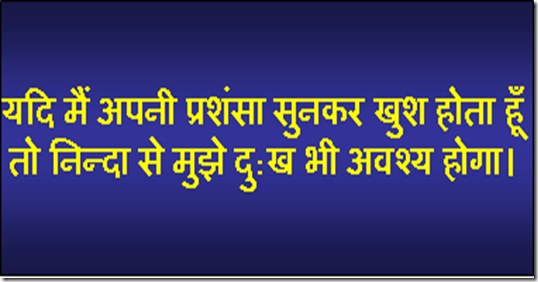 |
काव्य प्रयोजन (भाग-3)पाश्चात्य विद्वानों के विचार |
| पिछले दो पोस्टों मे हमने काव्य-सृजन का उद्देश्य और संस्कृत के आचार्यों के विचार की चर्चा की थी। संस्कृत के आचार्यों ने कहा था कि लोकमंगल और आनंद, यही कविता का “सकल प्रयोजन मौलिभूत” है। आइए अब इसी विषय पर पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा उसकी चर्चा करें।
यूनानी दार्शनिक प्लेटो का काल ई.पू. 427-347 का है। यह समय एथेन्स के पतन का था। इस समय आध्यात्मिक और नैतिक ह्रास में काफ़ी बढोत्तरी हुई। अतः उनकी चिन्ता थी कि कैसे आदर्श राज्य की स्थापना हो और चरित्र निर्माण द्वारा नैतिक मूल्यों की रक्षा कैसे हो? उन्होंने भी लोकमंगल, अर्थात् सत्य और शिव, के आधार पर काव्य के प्रयोजन को देखा। प्लेटो का मानना था कि काव्य का उद्देश्य मानव-प्रकृति में जो महान और शुभ है, नैतिक और न्यायपरायण है, उसका उसका उद्घाटन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने कला के आनंद सिद्धांत से आगे बढकर लोकमंगल सिद्धांत को महत्वपूर्ण बतया।
पाश्चात्य विद्वानों मे जिन्होंने काव्य प्रयोजन पर चर्चा की एक और महत्वपूर्ण नाम है लांजाइनस का। इन्होंने अपने ग्रंथ ‘परिइप्सुस’ में कहा है कि काव्य वाणी का ऐसा वैशिष्ट्य है, चरमोत्कर्ष है, जिससे महान कवियों को जीवन में प्रतिष्ठा और यश मिलता है। कारण यह है कि उसका सृजन, पाठक को मात्र जागृत करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके मन में अह्लाद उत्पन्न करने में सक्षम होता है। उनका मानना था कि महान सृजन महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लांजाइनस ने काव्य में उदात्त-तत्व की बात की थी। उदात्त की शक्ति से पाठक कृति-प्रभाव को ‘आत्मातिक्रमण’ के रूप में ग्रहण करता है। इसमें भी भाव-परिष्कार, भाव-उन्नयन या विरेचन सिद्धांत शामिल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य विचारकों ने लोकमंगलवादी (शिक्षा और ज्ञान) काव्यशास्त्र का समर्थन किया। महान काव्य वही है जो सभी को सब कालों मे आनंद प्रदान करे और समय जिसे पुराना न कर सके। इस प्रकार ‘आनंद’ या ‘आत्मातिक्रमण’ ही साहित्य का मुख्य प्रयोजन है। |
गुरुवार, 26 अगस्त 2010
संप्रेषण की समस्या
कभी-कभी ऐसा लगता है कि कविता का युग समाप्त हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है बौद्धिक सन्निपात से ग्रसित कविताओं की बहुतायात। यह बात तय है कि जहां कविताएँ बौद्धिक होगी, वहां वे शिथिल होगी। कविता की निर्मिति इसी जीव जगत से होती है। यदि कविता कुछ ही परिष्कृत बौद्धिक लोगों को प्रभावित या आकृष्ट करती है तो कही-न-कही कविता कमजोर अवश्य है। कविता की व्याप्ति इतनी बड़ी हो कि वे जन सामान्य को समेट सकें। आज कविता और पाठक के बीच दूरी बढ़ गई है। संवादहीनता के इस माहौल में संप्रेषण की समस्या पर विचार करने के लिए हमने डॉ० रमेश मोहन झा से निवेदन किया था। उन्होंने हमारे निवेदन ![[19012010014[4].jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV71RlwivX0bUmXCNZlqQALyZln-UzRaedL1Ot77dVkhJMevY2l8QErSz86vQUUoSvgcdramQHSRPnnLOaXoDcN1zGjNgG-Jfzm0NKf942YCDZeJWQI1S16_FyRPMFwazpw6P71I0V9z92/s1600/19012010014%5B4%5D.jpg) पर यह आलेख दिया है। उसे हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।
पर यह आलेख दिया है। उसे हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।
संप्रेषण की समस्या
काव्य की प्रारम्भिक अवस्था से ही कवियों के समक्ष अनुभूत सत्य को मार्मिक और प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने की समस्या बड़ी प्रमुख रही है। प्रत्येक युग का कवि कुछ विशिष्ट अनुभूतियाँ उपलब्ध कर उन्हें संपूर्णता में व्यक्त कर अपनी कला को सफल मानता है। काव्य की असफलता का कारण इन्हीं दो पक्षों – अनुभूति और अभिव्यक्ति में से किसी किसी एक का त्रुटिपूर्ण होना है।
यदि अनुभूति अपरिपक्व है तो उसके महत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रेष्ठ साहित्य के लिए अनुभूति की परिपक्वता का ही महत्व है उसके बिना न तो वस्तु का महत्व होगा और न शिल्प-साधना का प्रश्न सामने आएगा। अनुभूति की परिपक्वता पहली शर्त है। इसके बाद ही शिल्प का प्रश्न आता है, अतः शिल्प की पूर्णता श्रेष्ठ काव्य की दूसरी अनिवार्य शर्त्त है।
अनुभूति का उल्लेख होते ही उसमें बिना सोचे-समझे एक विशेषण “तीव्र” जोड़ दिया जाता है। लेकिन अनुभूति की तीव्रता का आशय क्या है, इसे कम लोग जानते हैं। अनुभूति की तीव्रता एक्साइटमेंट नहीं है। अज्ञेय ने ठीक ही कहा है –
भावनाएं नहीं है सोता
भावनाएँ खाद है केवल
जरा इनको दबा रखो
जरा सा और पकने दो
तले और तपने दो
अँधेरी तहों की पुट में
पिघलने और पकने दो
रिसने और रचने दो
कि उनका सार बनकर
चेतना की धरा को
कुछ उर्वर कर दे
- “हरी घास पर क्षण भर”
काव्य के लिए अनुभूतियों के शोध का बड़ा महत्व है। इसी से शैली में प्रभावोत्पादकता आती है। आवेश में सृजन संभव नहीं है। सृजन की स्थिति आवेश की स्थिति से नितांत भिन्न है।
सृजन के लिए धैर्य की नितांत आवश्यकता है। हड़बड़ाहट में सबकुछ कहने की चेष्टा में काव्य सूचना का जखीरा बन जाता है और काव्यात्मकता गुम हो जाती है। साथ ही धैर्य का अभाव और आवेश की अधिकता के कारण उनका अनुभूत सत्य कलात्मक ढंग से संप्रेषित होने से रह जाता है, भाषा भी फीलपाँवो वाली हो जाती है। अतः अनुभूत सत्य को संप्रेषित करने के लिए संयम अनिवार्य है। एक-एक शब्द तौल-मोलकर रखना है। अतः कवियों को चाहिए कि वे शब्दों का संधान, शोध और परिमार्जन करते रहें। इसके बिना वे श्रेष्ठ रचना रच नहीं सकते। उर्दू के शायर एक एक शब्द गढ़ने में पूरी ताकत या यों कहें कि भावों को सकेन्द्रित कर देते हैं तब जाकर एक शे’र कहते हैं, और उसकी गहराई देखकर लोग दाँतों तले उंगली दबा लेते हैं। उनके यहां इसे वज़न कहते हैं। हमारे यहां भी यह वज़न वाली शैली अपनानी चाहिए तभी कविता में जान आ पाएगी। अज्ञेय इस विषय में कहते हैं –
किसी को
शब्द हैं कंकड़
कूट लो पीस लो
छान लो डिबिया में डाल दो
किसी को
शब्द है सीपियाँ
लाखों का उलट फेर
कभी एक मोती मिल जाएगा।
-- “इन्द्रधनुष रौंदे हुए ये”
शब्दों के साथ-साथ बिम्बों का भी ज़िक्र जरूरी है। आज कविता में विम्बों की जो प्रधानता है उसका संबंध भी अनुभूत सत्य के संप्रेषण से है। बिम्बों की योजना अभिव्यक्ति को समर्थ और सार्थक बनाने का साधन या निमित्त है। यदि बिम्बों में सजीवता है तो उसका कारण अनुभूति की सत्यता और ईमानदारी है।
अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता के साथ-साथ अभिव्यक्ति की “एकुरेसी” कविता को पुष्ट और पूर्ण बनाती है। “एकुरेसी” को केंद्र में रखते हुए कविता के शब्दकोश में अत्यधिक व्याप्ति आ गई है। लोक से लेकर अनेक शास्त्रों की परिभाषिक शब्दावली को आयात किया गया है।
अब इसके प्रयोग की जिम्मेदारी कवियों पर है। इसे सहज ढंग से गूंथने से भाषा में स्पष्टता, बेधकता, अचूकता और सार्थकता को गुंफित किया जा सकता है। और वही काव्य श्रेष्ठ माना जाएगा जिसमें शब्द-शब्द धुला पूछा हो, उसमें शक्ति और सौन्दर्य दोनों का सम्मिश्रण हो।
बुधवार, 25 अगस्त 2010
कविता के नए सोपान (भाग–7) - निष्कर्ष
निष्कर्षकविता के नए सोपान (भाग–7) |
कविता के नए सोपान (भाग-1)कविता के नए सोपान (भाग-2) :: “कविता जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है।”कविता के नए सोपान (भाग-3) - कविता सिर्फ़ हृदय की मुक्तावस्था नहीं, बल्कि बुद्धि की मुक्तावस्था है।कविता के नए सोपान (भाग-4) आज का कवि परिवेश के साथ द्वंद्वमय स्थिति में है।कविता के नए सोपान (भाग-5) – कविता का निर्वैयक्तिकता सिद्धांतकविता के नए सोपान (भाग-6) काव्य चिंतन में नई समीक्षा |
| आज की कविता का आग्रह कठिन काव्यशास्त्र के प्रति नहीं रहा है। आज की कविता की खासियत यही है कि यह अत्यंत मुखर होकर पूरे साहस से अपने पाठकों, अपने श्रोताओं के समक्ष आ रही है। अधिकांश कविता आज एक रस है, तब भी आज भी कविता के संवेदन को, संघर्ष को, विचार को हम स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। पिछले छह भागों में प्रस्तुत विचारों पर गौर करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुराने प्रतिमान आज उतने कारगर नहीं रहे, जितने कि पहले थे। यहां तक कि रस अब कविता के लिए आवश्यक नहीं रह गया है। हालांकि छायावाद के आलोचक डॉ नगेन्द्र ने नए काव्य चिंतन के इस दौर में भी “कविता क्या है?” शीर्षक आलेख में रस सिद्धांत को काव्य का शाश्वत प्रतिमान माना है, किन्तु अज्ञेय ने इस सिद्धांत का खंडन किया। अज्ञेय का कहना था कि रस का आधार था अद्वंद्व और चित्त की समाहिति (शांति), जबकि नई कविता का आधार है तनाव, द्वंद्व। अज्ञेय का मानना था, “जीवन.... सपनों और आकारों का एक रंगीन और विस्मय भरा पुंज है। हम चाहें तो उस रूप से ही उलझे रह सकते हैं। पर रूप का आकर्षण भी वास्तव में जीवन के प्रति हमारे आकर्षण का प्रतिबिंब है। जीवन को सीधे न देखकर हम एक काँच में से देखते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम उन रूपों में ही अटक जाते हैं, जिनके द्वारा जीवन अभिव्यक्ति पाता है”।(अत्मनेपद) इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि नई कविता के संदर्भ में सिर्फ अनुभूति ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि यह तो भ्रम पैदा करती है। छायावादी कविता की अनुभूति और नई कविता की अनुभूति में बदलाव है। आज हम निर्वैयक्तिक अनुभूति की बात करते हैं। (यहां देखें) निरंतर प्रयोग में आते रहने से शब्द में बासीपन आ जाता है। इसलिए आज कवि के सामने शब्द में नया अर्थ भरने की चुनौती है। तो नया कवि इस चुनौती को स्वीकार कर शब्दों में नए अर्थ का निरूपण करता है। हम पहले भी इस बात की चर्चा कर आए हैं कि नई कविता “अभिव्यक्ति” नहीं है, निर्मित है। (यहां देखें) अगर विजयदेव नारायण साही के शब्दों में कहें तो नई कविता तरंग के रूप को स्ट्रक्चर में बदल देती है जेसे हीरे का क्रिस्टल हो। कविता निर्मित इसलिए है कि आज हमको कलाकृति कि संरचना पर ध्यान देना पड़ता है। आज कविता को परखने का प्रमाणिक प्रतिमान काव्य भाषा है। क्योंकि काव्य-भाषा ही वह चीज है जिसमें काव्यार्थ की, नए भाव-बोध की निष्पत्ति होती है। इस सारी चर्चा के निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जहां एक ओर आज कविता का ऊपरी कलेवर बदला है, साथ ही नए प्रतीकों या बिम्बों या शब्दावली की खोज हुई है, वहीं दूसरी ओर गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में ही फर्क आ गया है। इसका कारण है हमारे रागात्य संबंधें की प्रणालियाँ बदली है। इन रागात्मक प्रणालियों के बदलाव से हमारा बाह्य और आंतरिक वास्तविकता से गहरा रिश्ता निर्धारित होता है। जीवन आज जटिल हुआ है। इस काव्यानुभूति का कवि-कर्म पर गहरा असर पड़ा है। आज कविता हमें रिझाती नहीं, हमारा चैन तोड़ देती है। शब्द और अर्थ का तनाव स्पष्ट दीखता है। सृजन में नए नए अर्थ सौंदर्य की तलाश जारी है। वस्तु और रूप के बीच एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। |
मंगलवार, 24 अगस्त 2010
कविता के नए सोपान (भाग-6) काव्य चिंतन में नई समीक्षा
काव्य चिंतन में नई समीक्षाकविता के नए सोपान (भाग-6) |
| पाश्चात्य काव्य चिंतन में नई समीक्षा (न्यू क्रिटिसिज़्म) स्कूल के विद्वानों ने काव्य लक्षण पर बहस करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि “कविता एक शाब्दिक निर्मित है या वर्बल आईकॉन है(Verbal Icon) ” अर्थात् कविता शब्द है और अंत में भी यही बात बचती है कि कविता शब्द है। (यहां देखें) टी.एस.एलियट (यहां देखें) और अई.ए. रिचर्डस (यहां देखें ) इसी न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल से हैं। नई समीक्षा के विचारकों ने काव्य-भाषा को आधार बनाकर विचार किया। अर्थात इनकी समीक्षा में “कवि” केंद्र में नहीं है। इनके चिंतन का केंद्र “कविता” है। इस स्कूल के विचारकों द्वारा कविता का विश्लेषण काव्य-भाषा के आधार पर हुआ। उसकी कलाकृति की प्रक्रिया पर चिंतन किया गया। उन्होंने काव्य-भाषा को आधार बनाकर चिंतन किया। इस स्कूल में विचारकों का कहना था, “कविता भाषा की संभावित क्षमताओं का संधान है।” इस स्कूल का मानना था कि कविता के अर्थ पता लगाने की मूल समस्या भाषा की समस्या है। हिंदी आलोचना में न्यू क्रिटिसिज्म के पुरोधा अज्ञेय ने भी पाश्चात्य विद्धानों द्वारा दिए गए परिभाषा को बार बार दुहराया कि काव्य शब्द है। उन्होंने कहा कि शब्द का संस्कार ही कृतिकार को कृती बनाता है। अज्ञेय द्वारा कही गई बात का अन्य विद्वानों ने भी समर्थन दिया। डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी ने “भाषा और संवेदना”, “अज्ञेय : आधुनिक रचना की समस्या” में भी अज्ञेय द्वारा कही गई बात को समर्थन देते हुए कहा कि काव्य शब्द है और कविता को काव्य भाषा के आधार पर ही परखा जाना चाहिए। |
सोमवार, 23 अगस्त 2010
कविता के नए सोपान (भाग-5) – कविता का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत
कविता का निर्वैयक्तिकता सिद्धांतकविता के नए सोपान (भाग-5) |
| छायावादियों ने कविता की परिभाषा करते हुए “स्वानुभूति” पर बल दिया था। (यहां पढें) । वही दूसरी ओर नयी कविता के कवि-आलोचकों ने कहा कि परिवेश में बदलाव के कारण “अनुभूतिगत भिन्नता” है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करने से पहले, कवि, आलोचक और चिंतक विजयदेवनारायण साही की पंक्तिया उद्धृत करें,
अनुभूति की बनावट का फ़र्क़ ही छायावादी “स्वानुभूति” और नयी कविता की “अनुभूतिगत भिन्नता” के अन्तर को स्पष्ट करता है। कविता के नये प्रतिमान में इसी बात को बताते हुए प्रो. नामवर सिंह ने कहा है,
नयी कविताओं में कवि अनुभूति से अधिक अनुभूति के बदले हुए संदर्भ पर अधिक बल देते हैं। इसीलिए हम पाते हैं कि नयी कविताओं में कवि अनुभूति से अधिक अनुभूति के बदले हुए संदर्भ पर अधिक बल देते हैं। और यह भी स्पष्ट है कि उनका बल रागात्मक संबंधों पर है। कवि और चिंतक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयायन अज्ञेय का भी मानना था कि हमारे रागात्मक संबंधों में भी बदलाव आया है। इसके फलस्वरूप पुराने संस्कारगत रागात्मक संबंधो में बदलाव परिलक्षित है। (यहां पढें) अज्ञेय ने बात को और स्पष्ट करते हुए “दूसरा सप्तक” की भूमिका में कहा है,
कवि का क्षेत्र तो रागात्मक संबंधों का क्षेत्र होता ही है। इसलिए ये जो बदलाव है, उसका आज के कवि कर्म पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। हमारे चारो तरफ़ जो बाहरी वातावरण है, जैसे-जैसे उसमें परिवर्तन आता जाता है, वैसे-वैसे हमारे रागात्मक संबंध को जोड़ने की पद्धति भी बदलती जाती है। अगर ऐसा न हुआ होता, अगर बदलाव न हुआ होता, तो उस बाहरी वास्तविकता से तो हमारा नाता ही टूट जाता। अज्ञेय को पश्चिम में चल रहे एंटी रोमांटिक चिंतन का पता था। उस समय में पाश्चात्य सृजन की चिंतन धारा में एक नयी सोच शुरु हुई थी। उसका आधारभूत स्वर रोमांटिक भावबोध का विरोधी था। यहां पर
यह परिभाषा रोमांटिकों के “आत्माभिव्यक्ति” सिद्धांत का विरोध ही नहीं निषेध भी करती है। इन विचारों के साथ जो सिद्धांत सामने आया उसे “निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत” कहा गया। व्यक्तित्व से पलायन का अर्थ है अपने और पराए की भेद-बुद्धि से मुक्त हो जाना। निर्वैयक्तिक हो जाना। इसी अवस्था को भारतीय काव्यशास्त्र में कहा गया है,
|
रविवार, 22 अगस्त 2010
कविता के नए सोपान (भाग-4)
कविता के नए सोपान (भाग-4)आज का कवि परिवेश के साथ द्वंद्वमय स्थिति में है। |
कवि, आलोचक और चिंतक विजयदेवनारायण साही नई कविता के दौर के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उन्होंने नयी कविता के ऊपर अपने विचार रखते हुए कहा, “कविता कवि की भावनाओं तथा परिवेश के बीच संघर्ष की उपज है।” उनका यह मानना था कि यह संघर्ष कोई नई चीज नहीं है। यह पहले भी था। लेकिन उनका यह कहना था कि पहले का कवि अधिक “विदग्ध” (दक्ष) था। तात्पर्य यह कि वह कवि इस संघर्ष से न सिर्फ बचने के उपाय जानता था, बल्कि वह इस संघर्ष से उपजे तनाव से बच भी जाता था। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। आज का कवि अपने परिवेश के साथ एक द्वंद्वमय स्थिति जी रहा होता है। जिस परिवेश में हम रहे हैं उसमें भी बदलाव आया है। इस बदलाव के कारण अनुभूति की जटिलता बढ़ी है। संवेदनात्मक उलझाव का समावेश भी परिवेश में हुआ है। ये सारे तत्व आज की कविता को प्रभावित कर रहे हैं। इस जटिलता और उलझाव के कारण कविता के कलेवर में भी बदलाव आया है। इसके अलावा एक और चीज उल्लेखनीय है कि अगर गहरे स्तर पर देखें तो काव्यानुभूति की बनावट में भी फर्क आया है। चेतना के तत्व जो पहले की कविता में काव्यानुभूति के आवश्यक अंग थे, आज के दौर-दौरा में अनुपयोगी दिखने लगे हैं। लगता है इस बदलते परिवेश में वे सार्थक नहीं रहे। इसी तरह कुछ ऐसे तत्व जिन्हें पहले अनावश्यक माना जाता था, आज वे ही काव्यानुभूति के केंद्र में आ गए हैं। साही जी अपनी बात को एक निष्कर्ष तक लाते हुए “शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट” शीर्षक लेख में कहते हैं, “कुल मिलाकर काव्यानुभूति और जीवन की काव्येतर अनुभूतियों में जो रिश्ता दिखता था, वह रिश्ता भी बदल गया है।” इस प्रकार नई कविता में अनुभूति की बनावट की भिन्नता परिलक्षित है। अतः हम पाते हैं कि नए कवि अनुभूति से अधिक अनुभूति के परिवर्तित संदर्भ पर अधिक बल देते हैं। |
शनिवार, 21 अगस्त 2010
कविता के नए सोपान (भाग-3) - कविता सिर्फ़ हृदय की मुक्तावस्था नहीं, बल्कि बुद्धि की मुक्तावस्था है।
कविता के नए सोपान (भाग-3)कविता सिर्फ़ हृदय की मुक्तावस्था नहीं, बल्कि बुद्धि की मुक्तावस्था है। |
नयी कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुँवर नारायण अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक (१९५९) के प्रमुख कवियों में रहे हैं। 2009 में वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गए कुँवर नारायण ने तीसरा सप्तक के कवि-वक्तव्य में कहा,
यह परिभाषा कविता में रोमांटिक दृश्टि का विरोध करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुँवर नारायण एंटी रोमांटिक दॄष्टि का समर्थन करते हैं। यहां पर उन्होंने “मार्मिक अभिव्यक्ति” का प्रयोग किया है। कहीं न कहीं वो अज्ञेय के इस मत से कि “वास्तविकता के बदलते संदर्भ में नए रागात्मक संबंध की प्रमाणिकता के विकास की तथ्यगत स्थिति” के बहुत क़रीब है। इस परिभाषा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कविता सिर्फ़ भावना की अभिव्यक्ति नहीं है। वह बुद्धि से प्रेरित सर्जना है। यानी सिर्फ़ हृदय की मुक्तावस्था नहीं, बल्कि बुद्धि की मुक्तावस्था है। |
गुरुवार, 19 अगस्त 2010
कविता के नए सोपान (भाग-2) :: “कविता जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है।”
कविता के नए सोपान (भाग-2)“कविता जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है।” |
| प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, वह नई कविता है। जिनमें परंपरागत कविता से आगे नये भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नये मूल्यों और नये शिल्प-विधान का अन्वेषण किया गया। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा नयी कविता के प्रसिद्ध सिद्धांतकार और कवि हैं। इनकी रचना “नये प्रतिमान पुराने निकष”, “लक्ष्मीकांत वर्मा की प्रतिनिधि रचनाएँ” में संकलित हैं। उनका मानना था, अज्ञेय द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित 'तारसप्तक' के सात कवियों में से एक
इस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है। पहली यह कि नयी कविता जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। और दूसरी बात यह कि माथुर जी द्वारा यह भी कहा गया कि इन जटिल संवेदनाओं को सर्वग्राह्य और सम्प्रेषणीय बनाता है। अर्थात् कवि के विचारों का साधारनीकरण भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। |
बुधवार, 18 अगस्त 2010
कविता के नए सोपान (भाग-1)
कविता के नए सोपान (भाग-1)
नयी कविता के कवियों-अलोचकों ने काव्य को नए ढ़ंग से परिभाषित किया है। प्रयोगवाद के साथ-साथ नई कविता पर बहस चली। इस बहस में यह प्रश्न भी सामने आया कि “नया” क्या है? साथ ही यह भी विचारणीय रहा कि कविता क्या है?
आधुनिक हिन्दी कविता में डाक्टर जगदीश गुप्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनका मानना था कि,
“ये दोनों प्रश्न परस्पर सम्बद्ध और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि कविता में नवीनता की उत्पत्ति वस्तुतः सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से उत्पन्न होती है।”
बात सही भी है। कवि जो भी कहता है उसमें यदि सृजनात्मकता और संवेदनीयता नहीं हो, तो उसे कविता नहीं कहा जा सकता। “नई कविता स्वरूप और समस्याएं” पुस्तक में जगदीश गुप्त ने कहा कि
“ कविता सहज आंतरिक अनुशासन से युक्त अनुभूति जन्य सघन-लयात्मक शब्दार्थ है जिसमें सह-अनुभूति उत्पन्न करने की यथेष्ट क्षमता निहित रहती है।”
उन्होंने “यथेष्ट” शब्द का प्रयोग किया है। यथेष्ट शब्द कवि और पाठक दोनों को समाहित किए है। इसका अर्थ यह हुआ कि कविता के विषय में कवि का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। पाठक या श्रोता की मान्यता अनिवार्य है।
पर इस नई कविता को परिभाषित करते समय जगदीशगुप्त ने सृजनात्मकता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस कारण से कुछ विद्वानों ने इस परिभाषा पर आपत्ति भी उठाई है। जाने माने आलोचक डॉ. नामवर सिंह ने, “कविता के नए प्रतिमान” में “कविता क्या है” निबंध लिखा है। इस निबंध में उन्होंने कहा,
“डॉ. जगदीशगुप्त अपनी काव्य-परिभाषा में वह तत्व भूल गए जिसे नई कविता ने हिंदी काव्य-परम्परा से जोड़ा है। इसलिए अनुभूति तो उन्हें याद रह गई लेकिन सृजनात्मकता भूल गए।
“जगदीशगुप्त की परिभाषा की यह सबसे बड़ी सीमा है। यह परिभाषा छायावादी अनुभूति और नई कविता की नई अनुभूति में फर्क करके नहीं चलती।”
“सह-अनुभूति” में विचार-भंगिमा का नयापन है। “सह अनुभूति” , “रसानुभूति” का पर्याय नहीं है। यह नवीन काव्यानुभूति का पर्याय है। अतः हम कह सकते हैं कि सह-अनुभूति का प्रश्न रसानुभूति के विरोध में उठाया गया था।
मंगलवार, 17 अगस्त 2010
काव्य के मूल में मानवीय संवेदना की सक्रियता है।
"काव्य के मूल में मानवीय संवेदना की सक्रियता है।” |
| नई कविता के कवियों ने काव्य को नए ढंग से परिभाषित किया। उन्होंने रचनाओं में संवेदनशीलता पर उन्होंने विचार किया। इन आलोचकों कवियों का कहना था कि काव्य के मूल में मानवीय संवेदना ही सक्रिय रहती है। जिस तरह से हमारा जीवन गतिशील और परिवर्तनशील है, उसी तरह मानवीय संवेदना भी है। हमारे आसपास जो कुछ है, जो घटित हो रहा है उसका प्रभाव काव्य पर पड़ना स्वाभाविक है। परिवेश की नवीनता, उसका बदलाव, काव्य चिंतन के परिप्रेक्ष्य को बदल देती है।
रघुवीर सहाय के काव्य संकलन सीढि़यों पर धूप में की भूमिका में अज्ञेय ने कहा है - “काव्य सबसे पहले शब्द है। और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है।" यह एक महत्वूपर्ण परिभाषा है। सारे कविधर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं। शब्द का ज्ञान और इसकी अर्थवत्ता की सही पकड़ से ही एक व्यक्ति रचनाकार से रचयिता बनता है। अज्ञेय का मानना था कि ध्वनि, लय छंद आदि के सभी प्रश्न इसी में से निकलते हैं और इसी में विलय होते हैं। अज्ञेय तो यहां तक कहते हैं कि “सारे सामाजिक संदर्भ भी यहीं से निकलते है। इसी में युग-सम्पृक्ति का और कृतिकार के सामाजिक उत्तरदायित्व का हल मिलता है या मिल सकता है।" इस प्रकार जब हम काव्य लक्षण परम्परा की चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पाते हैं कि या तो काव्यार्थ शब्द में है या अर्थ में है या फिर दोनों में है। इस बहस में एक बात तो स्पष्ट है कि अधिकांश आचार्यों ने शब्द पंरपरा का ही समर्थन किया है। दूसरी प्रमुख बात जो सामने आती है वह यह है कि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस जैसे पुराने प्रतिमान, जिस तरह से पहले कारगर थे आज नहीं रहे हैं। |
सोमवार, 16 अगस्त 2010
कविता सामूहिक भाव बोध की अभिव्यक्ति है।
"कविता सामूहिक भाव बोध की अभिव्यक्ति है।”हिंदी की चिंतन परंपरा में काव्य लक्षणभाग – 5 प्रगतिवाद काल |
| काव्य चिंतन को प्रगतिवादियों ने नए ढंग से उठाया। इस धारा के विद्वानों का मानना था कि कविता विकासमान सामाजिक वस्तु है। इसका सृजन तो व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सृजन मूलतः सामाजिक और सांस्कृतिक भूमि पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कविता में संस्कृतिक परंपराओं की संवेदना समाहित होती है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नयी कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध में इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। प्रगतिवादी काव्य प्रक्रिया को छायावादी काव्य प्रक्रिया से अलग मानते है। मुक्तिबोध का मानना था कि – “इसका अर्थ यह नहीं है कि आज का कवि व्याकुलता या आवेश का अनुभव नहीं करता। होता यह है कि वह अपने आवेश या व्याकुलता को बांधकर, नियंत्रित कर, ऊपर उठाकर, उसे ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में या संवेदनात्मक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर देता है।”
“रोमैंटिक कवियों की भांति आवेशयुक्त होकर, आज का कवि भावों को अनायास स्वच्छंद अप्रतिहत प्रवाह में नहीं बहता। इसके विपरीत, वह किन्ही अनुभूत मानसिक प्रतिक्रियाओं को ही व्यक्त करता है। कभी वह इन प्रतिक्रियाओं की मानसिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, कभी वह उस रूप रेखा में रंग भर देता है।” मुक्तिबोध ने आगे यह कहा कि “इसका अर्थ यह नहीं है कि आज का कवि व्याकुलता या आवेश का अनुभव नहीं करता। होता यह है कि वह अपने आवेश या व्याकुलता को बांधकर, नियंत्रित कर, ऊपर उठाकर, उसे ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में या संवेदनात्मक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर देता है।” मुक्तिबोध का काव्य को "सांस्कृतिक प्रक्रिया" कहने के पीछे यह तर्क है कि काव्य-सृजन में सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक शक्तियों का हाथ होता है इस लिए यह सांस्कृतिक प्रक्रिया है। यह तो स्पष्ट है कि प्रगतिवाद का काव्य चिंतन मार्क्सवाद से प्रभावित है। वे यह अवष्य मानते हैं कि काव्यानुभूति की बनावट में सामाजिक सौंदर्यानुभूति की भूमिका अहम है।
“काव्य एक महान सामाजिक क्रिया है – जो सामाजिक विकास के समानांतर विकसित होती रहती है।” इस परिभाषा से यह सिद्ध होता है कि कविता सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती है । पाश्चात्य चिंतक काडवेल का "Illusion and Reality" में कहना था "Art is the product of society as the pearl is the product of the oyster." अर्थात "साहित्य वह मोती है जो समाज रूपी मोती तें पलता है।” उसके इस कथन को अधिकांश प्रगतिवादी मानते रहे। यह एक भौतिकवादी चिंतन है। कविता में जिस अनुभूति का चित्रण होता है वह वैयक्तिक न होकर भी सामाजिक होती है। इस सामाजिक अनुभूति में जटिलता, संश्लिष्टता और तनाव रहता है। इससे हटकर जार्ज लुकाच ने द्वंद्वात्मक भातिकवादी विचारधार को आगे बढ़ाया। उनका कहना था “हमारी चेतना मात्र भौतिक स्थितियों से नियंत्रित नहीं होती वह अपेक्षाकृत स्वतंत्र है और कभी कभी वह बाहरी भौतिक स्थितियों के विपरीत भी जा सकती है।” यह दृष्टि सौंदर्यशास्त्रियों के चिंतन से बहुत मेल खाती है। ऊपर कही गई बातों पर गौर करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कविता में जिस अनुभूति का चित्रण होता है वह वैयक्तिक न होकर भी सामाजिक होती है। इस सामाजिक अनुभूति में जटिलता, संश्लिष्टता और तनाव रहता है। इसलिए हम निष्कर्ष के रूप में यह मान सकते हैं कि कविता सामूहिक भाव बोध की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि ज्ञान-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार होता है। उनकी यह मान्यता प्रगतिवादियों को भी मान्य रही है। |
शुक्रवार, 13 अगस्त 2010
"काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है”
"काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है”हिंदी की चिंतन परंपरा में काव्य लक्षणभाग – 4 :: छायावाद काल |
| हिंदी साहित्य में यह वह काल था जब निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी सक्रिय थे। छायावादी कवियों ने काव्य लक्षण पर नए ढंग से विचार किया।
"तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कान्तकामिनी कविता" प्रसाद, पंत और महादेवी भी यह अवधारणा व्यक्त करते रहे कि "काव्य अभिव्यक्ति है "। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक प्रमुख स्तंभों में से एक थे। वे सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा की जड़ से जोड़कर कविता को देखते थे। उन्होंने “काव्य और कला तथा अन्य निबंध” में काव्य को आत्मा की "संकल्पनात्मक अनुभूति" कहा। उनका कहना था -
इस परिभाषा में सौंदर्य और सत्य के सामंजस्य के लिए प्रतिभा से उपजी (प्रातिभ) अनुभूति पर विशेष बल दिया गया है। इस परिभाषा में हमें आचार्य शुक्ल की परिभाषा की झलक दीखती है। आचार्य शुक्ल का कविता को भाव-योग कहना (यहां देखें) और प्रसाद का अनुभूति-योग मानना सहमति ही तो दर्शाता है। इन दोनों की परिभाषा में पश्चिम के स्वच्छंदतावादियों का प्रभाव कम या न के बराबर था। ये दोनों कवि अपनी काव्य-चिंतन भूमि पर खड़े रहकर पश्चिम के काव्य-चिंतन का अर्थ ग्रहण कर रहे थे। कई बार छायावाद को स्वचंछंदतावाद का पर्याय मान लिया जाता है। शायद भ्रमवश। दोनों वाद अलग-अलग देशों में उपजे। इनका काल भी अलग-अलग था और ये अलग-अलग संस्कृति के काव्य-आंदोलन रहे। हां ऐसा प्रतीत होता है कि छायावाद के कवि-आलोचकों ने पश्चिम के विचारों को पढ़ा और समझा तो पर उसकी नकल नहीं की। इसे हम संयोग मान सकते हैं कि छायावादियों द्वारा कहा गया "मुक्ति की आकांक्षा " और "स्वानुभूति का विस्तार", स्वच्छंदतावादियों का भी केंद्रीय तत्व रहा। हमने वर्डसवर्थ की काव्य परिभाषा (यहां देखें) और कॉलरिंग की परिभाषा (यहां देखे) की चर्चा करते हुए देखा था कि इसका मूल आधार "भावना", “कल्पना” के योग से निकला काव्य है। वहीं दूसरी ओर छायावाद आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसमें वैयक्तिक अनुभूति पर अधिक बल दिया गया है। इस लिए हम कह सकते हैं कि छायावादियों की दृष्टि कवि-केंद्रित है, काव्य-केंद्रित नहीं। इस मत का आगे चलकर विरोध भी हुआ, जब प्रगतिवाद और नई कविता का काल आया। |
गुरुवार, 12 अगस्त 2010
“कविता हृदय की मुक्तावस्था है” :: हिंदी की चिंतन परंपरा में काव्य लक्षण-भाग – 3 नवजागरण काल – आचार्य रामचंद्र शुक्ल
“कविता हृदय की मुक्तावस्था है”हिंदी की चिंतन परंपरा में काव्य लक्षणभाग – 3 :: नवजागरण काल – आचार्य रामचंद्र शुक्लआचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक चिंतामणि में “कविता क्या है” निबंध लिखा इस निबंध को आचार्य शुक्ल जीवन भर लिखते परिस्कृत करते रहे। नवजागरण कालीन (भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग) मानसिकता का सबसे प्रबल विस्फोट इस निबंध में देखने को मिलता है। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने कविता के संबंध में अपना मत देते हुए कहा –
आचार्य शुक्ल यह भी कहते हैं कि इस साधना को हम भावायोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं। इस परिभाषा में जो विशेष बात है वह है रसदशा। रसदशा, उनके अनुसार हृदय की मुक्त अवस्था है। मुक्त हृदय को अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं,
ऐसा मुक्त हृदय प्राणी जब अपने हृदय को लोक-हृदय से मिला देता है तो यह दशा ही रसदशा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में रस दशा “हृदय की मुक्तावस्था” ही है। आचार्य शुक्ल ने कविता को “शब्द-विधान” की शक्ति माना। हमने पहले पाशचात्य काव्य शास्त्र की चर्चा करते हुए (लिंक यहां है) कहा था कि “नई समीक्षा” (न्यू क्रिटिसिज्म) स्कूल के विद्वानों ने काव्य लक्षण पर निष्कर्षतः कहा कि “कविता एक शाब्दिक निर्मित है” अर्थात कविता शब्द है और अंत में भी यही बात बचती है कि कविता शब्द है। कहीं न कहीं इस उक्ति में भी भारतीय चिंतन-परंपरा की ध्वनि मौजूद है। |

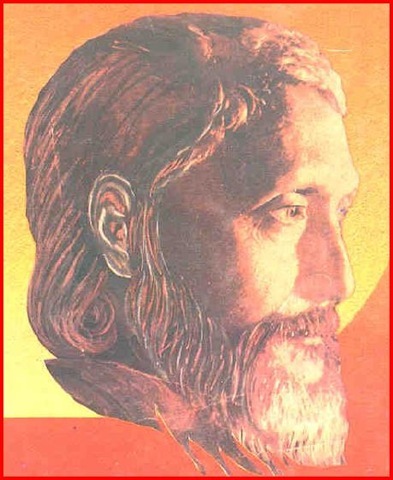 जिस प्रकार पाश्चात्य साहित्य के स्वच्छंदतावादी कवि ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि "कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन है" उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" ने कहा कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है –
जिस प्रकार पाश्चात्य साहित्य के स्वच्छंदतावादी कवि ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि "कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन है" उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" ने कहा कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है –