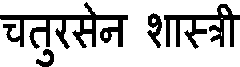मंगलवार, 21 अगस्त 2012
मंगलवार, 4 अक्टूबर 2011
ले चल मुझे भुलावा देकर
जयशंकर प्रसाद की कविताएं-3
ले चल मुझे भुलावा देकर
ले चल मुझे भुलावा देकर,
मेरे नाविक! धीरे-धीरे!
जिस निर्जन में सागर लहरी
अम्बर के कानों में गहरी --
निश्छल प्रेम-कथा कहती हो,
तज कोलाहल की अवनी रे!
जहां सांझ-सी जीवन छाया
ढीले अपनी कोमल काया,
नील नयन से ढलकाती हो,
ताराओं की पांति घनी रे!
जिस गम्भीर मधुर छाया में --
विश्व चित्र-पट चल माया में --
विभुता विभु-सी पड़े दिखाई
दुःख-सुख वाली सत्य बनी रे!
श्रम-विश्राम क्षितिज-वेला से --
जहां सृजन करते मेला से --
अमर जागरण-उषा नयन से --
बिखराती हो ज्योति घनी रे!
रविवार, 21 अगस्त 2011
प्रसाद जी की नाट्य संबंधी सोच
नाटक साहित्य-11
नाटक साहित्य – प्रसाद युग-4
प्रसाद जी की नाट्य संबंधी सोच
प्रसाद जी ने ‘हिंदी नाटक का स्थान’, ‘नाटकों में रस का प्रयोग’, ‘नाटकों का आरंभ’ और ‘रंगमंच’ नामक अपने लेखों में नाटक और रंगमंच पर विचार किया है। जब उन्होंने नाटक लिखना शुरु किया था तब हिंदी में नाटकों की समृद्ध परंपरा नहीं थी। भारतेन्दु युग के नाटक उनके सामने थे। इसके साथ ही संस्कृत और पश्चिम के नाटकों की समृद्ध परंपरा भी मौज़ूद थी। उन्होंने संस्कृत के नाटकों और नाट्य संबंधी अवधारणाओं का गहरा अध्ययन किया। पश्चिम के नाट्य चिंतन और परंपराओं से भी वे वाकिफ़ थे। उस समय के रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटकों पर पश्चिम के नाटकों का गहरा प्रभाव था। उस समय एक तो शिक्षित समाज के लिए अभिजात्य नाटक खेले जाते थे वहीं दूसरी तरफ़ जनसाधारण के पारसी रंगमंच के नाटक थे। प्रसाद हिंदी पर पारसी रंगमंच के प्रभाव को अच्छा नहीं मानते थे। वे अपनी नाट्य परंपरा के अनुरूप हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास के समर्थक थे।
प्रसाद जी नाटक को ‘कला का विकसित रूप’ मानते थे। वे नाटक को ‘सब ललित सुकुमार कलाओं का समन्वय’ कहते थे। नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों कलाओं की अनुभूति होती है। इसलिए वे यह नहीं चाहते थे कि लोग नाटक को देखते वक़्त खुद को भूल जाएं और तल्लीन हो जाएं। प्रसाद जी नाटकीयता और सोद्देश्यता दोनों को नाटक के लिए ज़रूरी मानते थे। वे कहते थे, “जो नाटक मनोभाव का विश्लेषण करके चमत्कार के बल से मोहता हुआ, अंतःकरण में आदर्श सत्य को स्वयंमेव विकसित कर देता है, उसे ... सभी सभ्य जातियों के साहित्य में सम्मान मिलता है।”
प्रसाद जी के अनुसार पश्चिम में कला को अनुकरण माना जाता है जबकि हमारे यहां कला में दार्शनिक सत्य की प्रतिष्ठा की जाती है। आत्मा का अभिनय भाव है। भाव ही आत्म-चैतन्य में विश्रान्ति पा जाने पर रस होते हैं। जैसे विश्व के भीतर से विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसी तरह नाटकों से रस की। भरत के अनुसार नाटक देखते हुए जो हृदय स्थित भाव है, वही परिपक्व होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। जब अभिनेता अपने आत्म चैतन्य में तल्लीन हो जाता है तो उसका भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार पश्चिम में नाटक के केन्द्र में अनुकरण होता है जबकि भारत में रस। इसलिए प्रायः भारत में नाटकों का अंत सुख या आनंद में होता है जबकि पश्चिम में दुखांत।
पश्चिम के नाटकों में त्रासदी का ज़ोर रहा तो इसीलिए कि उनकी परिस्थिति ने उन्हें लगातार दुख और संघर्ष की ओर अग्रसर किया। उपनिवेशों की खोज में दुर्गम भूभागों में उन्हें भटकना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन जीना पड़ा। इसीलिए उन्होंने जीवन को दुखमय (ट्रेजेडी) समझ लिया। चूंकि उन्होंने भावना की बजाए बुद्धि पर अधिक भरोसा किया इसलिए उन्होंने इस दुख को ही जीवन का सत्य समझ लिया।
बुद्धिवाद और दुख को (ट्रेजेडी) प्रधानता देने के कारण ही पश्चिमी सिद्धांत मनुष्य के चरित्र-निर्माण का पक्षपाती है। नाटक देखकर या कविता पढ़कर यदि मनुष्य अपने को बुराई की तरफ़ जाने से रोकता है और अपने चरित्र में संशोधन करता है तो साहित्य का लक्ष्य पूरा हो जाता है। मौज़ूदा साहित्य की दो प्रमुख विशेषताओं – व्यक्ति-वैचित्र्य और यथार्थवाद को इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। प्रसाद पाश्चात्य के व्यक्ति-वैचित्र्य को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। किन्तु उन्होंने आदर्शवाद को भी अंतिम नहीं माना है। उनके शब्दों में, “चरित्र-चित्रण आदर्श के लिए हो, यह अति उत्तम सिद्धांत नहीं है, क्योंकि चरित्र-चित्रण का लक्ष्य आदर्श तो अवश्य है, किन्तु प्रत्येक चरित्र आदर्श हो तो वही उपर्युक्त दोषापत्ति हो जाती है।” प्रसाद ने पात्र के ‘नैतिक विकास’ अर्थात् व्यक्तित्व के सहज विकास को मुख्यता दी है।
पश्चिम के विपरीत भारतीय परंपरा रस पर आधारित है। इसका कारण यह है कि पश्चिम की तरह आर्यों को घरबार छोड़कर इधर-उधर भटकना न पड़ा। भारतीय आर्य निराशावादी नहीं थे। उन्होंने प्रत्येक भावना में अभेद निर्विकार, अनंद लेने में अधिक सुख माना। रस में लोकमंगल की भावना प्रच्छन्न रूप में विद्यमान रहती है। भारतीय परंपरा में लोकमंगल स्थूल सामाजिक रूप में नहीं बल्कि दार्शनिक सूक्ष्मता के आधार पर मौज़ूद रहता है। जबकि पश्चिम में वासना का आधार रहता है। वासना से ही क्रिया संपन्न होती है। क्रिया के संकलन से व्यक्ति का चरित्र बनता है। चरित्र में महत्ता का आरोप हो जाने पर, व्यक्तिवाद का वैचित्र्य उस महती लीलाओं से विद्रोह करता है। इस प्रकार पश्चिम का साहित्य व्यक्ति और समाज की वासनात्मक क्रियाओं से ही संचालित और प्रेरित होता है। यही कारण है कि उसमें किसी दार्शनिक श्रेष्ठता के दर्शन नहीं होते।
आत्माभिव्यक्ति की गीतात्मकता को प्रसाद ने रसानुभूति माना है। रसवाद को अपनाने के कारण मनुष्य की वासनात्मक मनोवृत्तियां साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं। इससे मनुष्य की वासना का संशोधन हो जाता है। इससे मनुष्य की विशिष्टता और विभिन्नता समाप्त हो जाती है। मनुष्य की भावनाओं को मानवीय आधार मिल जाता है। इस आधार हम पाते हैं कि प्रसाद जी नाट्य रचना के लिए पश्चिम के अनुकरण सिद्धांत, बुद्धिवाद और दुख व निराशा को स्वीकार नहीं करते। वे नाटक में लोकमंगल को स्वीकार करते हुए भी रस को ही उसका लक्ष्य मानते हैं। प्रसाद द्वारा विवेचित ‘रसानुभूति’ ही ‘रंगानुभूति’ और ‘जीवनानुभूति’ है, क्योंकि उन्होंने रस का विवेचन ‘नाट्य’ और जीवन-संदर्भों के साथ जोड़ते हुए किया है। एक तरह से वे रस पर विचार करते हुए यथार्थवाद की अपनी परंपरा को तलाशते हैं।
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रसाद ने अनेक भारतीय रंग-परंपराओं की युक्तियों, रूढ़ियों और व्यवहारों का रचनात्मक उपयोग किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने आंशिक रूप से इन्हें नए संदर्भों में स्वीकारा, और कहीं-कहीं नकारा भी है। उनकी यह स्वीकृति न तो विवशता थी और न ही अस्वीकृति महज़ फैशन। वे अपनी विषय-वस्तु के अनुकूल रंग-तत्वों की तलाश करते रहे, जो विशुद्ध मनोरंजन से हटकर नए जीवन-बोध को अनेक आयामों के साथ व्यंजित कर सकें। इस पुनर्रचना के तहत उन्होंने न तो संस्कृत नाटकों के शास्त्रीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया है, न पारसी नाटकों की अतिनाटकीयता को पूर्णतया स्वीकार किया है, न इब्सन की तरह नाटकों को तर्कमूलक बनाया है और न ही शेक्सपियर के त्रासदी नाटकों से आतंकित हुए हैं।
***
संदर्भ ग्रंथ
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास – सं. डॉ. नगेन्द्र, सह सं. डॉ. हरदयाल २. डॉ. नगेन्द्र ग्रंथावली – खंड ९ ३. हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास – हजारीप्रसाद द्विवेदी ४. हिन्दी साहित्य का इतिहास – डॉ. श्यम चन्द्र कपूर ५. हिन्दी साहित्य का इतिहास – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ६. मोहन राकेश, रंग-शिल्प और प्रदर्शन – डॉ. जयदेव तनेजा ७. हिन्दी नाटक : उद्भव और विकास – डॉ. दशरथ ओझा ८. रंग दर्शन – नेमिचन्द्र जैन ९. कोणार्क – जगदीश चन्द्र माथुर १०. जयशंकर प्रसाद : रंगदृष्टि नाटक के लिए रंगमंच – महेश आनंद ११. अन्धेर नगरी में भारतेन्दु के व्यक्तित्व के स र्जनात्मक बिन्दु – गिरिश रस्तोगी, रीडर, हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्व विद्यालय १२. रंगमंच का सौन्दर्यशास्त्र – देवेन्द्र राज अंकुर १३. दूसरे नाट्यशास्त्र की खोज - देवेन्द्र राज अंकुर
रविवार, 14 अगस्त 2011
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से
जयशंकर प्रसाद की कविता - 1
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयंप्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती
अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो
प्रशस्त पुण्य पंथ हैं - बढ़े चलो बढ़े चलो ॥
असंख्य कीर्ति-रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह-सी
सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी
अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़वाग्नि से जलो
प्रवीर हो जयी बनो - बढ़े चलो बढ़े चलो
प्रसाद जी की नाट्य-रचनाएं
शनिवार, 13 अगस्त 2011
नाटक साहित्य – प्रसाद युग-2
सोमवार, 8 अगस्त 2011
आह ! वेदना मिली विदाई …. जयशंकर प्रसाद
मैंने भ्रमवश जीवन संचित,
मधुकरियों की भीख लुटाई
छलछल थे संध्या के श्रमकण
आँसू-से गिरते थे प्रतिक्षण
मेरी यात्रा पर लेती थी
नीरवता अनंत अँगड़ाई
श्रमित स्वप्न की मधुमाया में
गहन-विपिन की तरु छाया में
पथिक उनींदी श्रुति में किसने
यह विहाग की तान उठाई
लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी
रही बचाए फिरती कब की
मेरी आशा आह ! बावली
तूने खो दी सकल कमाई
चढ़कर मेरे जीवन-रथ पर
प्रलय चल रहा अपने पथ पर
मैंने निज दुर्बल पद-बल पर
उससे हारी-होड़ लगाई
लौटा लो यह अपनी थाती
मेरी करुणा हा-हा खाती
विश्व ! न सँभलेगी यह मुझसे
इसने मन की लाज गँवाई
गुरुवार, 5 मई 2011
प्रकृतवादी उपन्यास
मनोज कुमार
प्रकृतवाद एक विशिष्ट जीवन दर्शन है। यह मानव जीवन को वैज्ञनिक दृष्टि से प्रकृत रूप में (नेचुरल) देखने और चित्रित करने में विश्वास रखता है। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति का उसी प्रकार से क्रमशः विकसित जन्तु है, जिस प्रकार संसार के अन्य प्राणी। उसमें पशु-सुलभ सभी आकर्षण-विकर्षण ज्यों-के-त्यों वर्तमान हैं। प्रकृतवादी लेखक मनुष्य को काम-क्रोध आदि मनोरोगों का गट्ठर मात्र समझता है, और उसके अर्थहीन आचरणों, कामासक्त चेष्टाओं और अहंकार से उत्पन्न धार्मिक वृत्तियों का विशेष भाव से उल्लेख करता है। इस विचार धारा के अनुसार जीवन में जिसे विद्रूप और कुत्सित कहा जाता है, वह सहज और वैज्ञानिक भी है। इस विचार धारा के जनक ज़ोला का मानना है,
“लेखकों का धर्म है कि वे जीवन के गंदे और कुरूप से कुरूप चित्र खींचे। मनुष्य की दुर्बलताओं, रोगों और विकृतियों का वर्णन करते समय उन्हें कोई अंश नहीं छोड़ना चाहिए।”
समाज के पाखंडपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने वाले उपन्यासों के रचनाकरों में प्रमुख हैं –
चतुरसेन शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के चांदोख नामक गांव में 1891 में हुआ। ग्यारह वर्ष की अवस्था में वे वाराणसी पहुंच गए और वहां व्याकरण तथा साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने साहित्य लेखन को भी व्यवसाय बनाया। जयपुर संस्कृत कॉलेज में आयुर्वेद और संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया।
`हृदय की परख’ (1918), `हृदय की प्यास’ (1932), ‘वैशाली की नगरवधू’, ‘सोना और ख़ून’, ‘गोली’ ‘सोमनाथ’, ‘खग्रास’, ‘व्यभिचार’, `अमर अभिलाषा’ (1932), `आत्मदाह’ (1937), वयं रक्षाम, मन्दिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, आलमगीर, सह्यद्रि की चट्टानें, आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।
उपन्यासों के अलावा उन्होंने कहानियां भी लिखीं हैं और उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं – रजकण, अक्षत आदि।
पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ के ‘जिजा जी’, ‘दिल्ली का दलाल’ (1927), ‘चॉकलेट’, ‘चन्द हसीनों के खुतूत’ (1927), ‘बुधुआ की बेटी’ (1928), ‘शराबी’ (1930), ‘सरकार तुम्हारी आंखों में’ आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ‘उग्र’ जी की ‘बुधुआ की बेटी’ उपन्यास घोर यथार्थवादी उपन्यास है। ‘चन्द हसीनों के खुतूत’ पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिन्दी का पहला उपन्यास है।
‘उग्र’ जी अपने साहित्य में भी उग्र रूप में ही प्रकट हुए हैं। डॉ. गोपाल राय का कहना है,
“‘उग्र’ जी इस युग के सबसे अक्खड़ और सबसे बदनाम उपन्यासकार थे।”
‘चॉकलेट’ में अश्लीलता को लेकर उस ज़माने में हिंदी साहित्य जगत में विवाद खड़ा हो गया था। अपने उपन्यासों द्वारा उन्होंने समाज की बुराइयों को, उसकी नंगी सचाई को, बिना किसी लाग-लपेट के प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज के उपेक्षित, निचले तबके के लोग, पतित, को अपने उपन्यास का विषय बनाया, और उसके चित्रण में उन्होंने किसी प्रकार के ‘शील’ या ‘अभिजात्य शिष्टता’ का परिचय नहीं दिया। उनके उपन्यासों में सच्चाई नग्न रूप में आती है। वे समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाजसुधार, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता की ओट में होनेवाले पाखंडपूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लानेवाली कथानक गढते हैं। उनकी भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षक वैचित्र्य के साथ चलती है। उनके उपन्यास ‘परचेबाज़ी’ के अधिक निकट दिखते हैं, जिसके कारण उनकी कोई भी कृति कलारूप को ग्रहण नहीं कर पाती। हालाकि उनके सभी उपन्यास सुधारवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, फिर भी सपाटबयानी और कम उम्र के पाठकों की रुचि को विकृत करने के खतरे से युक्त होने के कारण उनका सुधारवादी उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया।
ऋषभचरण जैन : के प्रमुख उपन्यास हैं ‘वैश्यापुत्र’, ‘मास्टर साहब’, ‘सत्याग्रह’, ‘बुर्क़ेवाली’, ‘चांदनी रात’, ‘दिल्ली का कलंक’, ‘दिल्ली का व्यभिचार’, ‘रहस्यमयी’, ‘हर हाईनेस’, ‘दुराचार के अड्डे’, ‘मयख़ाना’। उन्होंने तत्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर प्रकृतवादी उपन्यास लिखा और यथार्थ के नाम पर मानव जीवन की विकृतियों का खुलकर वर्णन किया है।
अनूपलाल मंडल : उन्होंने ‘निर्वासिता’ (1929) के अलावा पत्रात्मक प्रविधि में ‘समाज की बेदी पर’ और ‘रूपरेखा’ शीर्षक उपन्यास लिखे।
जयशंकर प्रसाद ने ‘कंकाल’ (1929) और ‘तितली’ (1934) की रचना द्वारा उपन्यासकार के रूप में भी चर्चा का विषय बने। ‘तितली’ में ग्रामीण और कृषक जीवन का वर्णन है। ‘कंकाल’ में उन्होंने समाज के त्यागे हुए, अवैध और अज्ञात-कुलशील संतानों की कथा कही है। इस उपन्यास का विषय प्रकृतवादी है। हालाकि उनकी दृष्टि सामाजिक है, फिर भी इस उपन्यास में कुछ व्यक्ति ही प्रधान बन गए हैं। ये व्यक्ति समाज में अकेले हैं। इनका कोई वर्ग नहीं है। स्वभाव से ये पात्र असामान्य हैं। प्रसाद समाज के इन उपेक्षित और लांछित व्यक्तियों के मसीहा बन कर उपस्थित होते हैं, और इनको केन्द्र में रखकर कहानी गढ़ते हैं। प्रसाद की कलम का असर है कि पाठक की करुणा इनके प्रति जगती है। लेकिन कहानी घटनाओं और चमत्कारों पर आधारित होने के कारण कृत्रिम और अविश्वसनीय लगती है। दूसरी बात कि प्रसाद की भाषा उपन्यासोचित नहीं है। इन कारणों से उपन्यासकार के रूप में प्रसाद बहुत सफल नहीं रहे। भाषा को अलंकृत करने का मोह वो त्याग न सके। भाषा को लक्षणा शक्ति से सजाने के कारण वह विषय से अलग लगने लगती है। इसलिए गोपाल राय कहते हैं,
“प्रतिभा-संपन्न लेखक होते हुए भी प्रसाद हिन्दी-उपन्यास को कोई नया आयाम नहीं दे सके।”
प्रकृतवादी उपन्यासकारों ने जीवन का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जिसे पढ़कर वितृष्णा पैदा होती है। ऐसा महसूस होता है कि जीवन में सब कुछ विद्रूप, कुत्सित और वीभत्स है। इस प्रवृत्ति को अधिक प्रश्रय नहीं मिला।
बुधवार, 20 अक्टूबर 2010
काव्य प्रयोजन :: आधुनिक काल
काव्य प्रयोजन :: आधुनिक काल |
द्विवेदी युग |
|
|
|
|
|
|
|
महादेवी वर्मा के अनुसार साहित्य का उद्देश्य है मानव करुणा का विस्तार। |
| प्रगतिवाद ने रूढिवादिता का विरोध किया और मार्क्सवादी समाज-चिंतन को अपनाया।
|
| नयीकविता युग तथा समकालीन युग के विद्वानों, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा आदि, कवियों के मतानुसार साहित्य का प्रयोजन मानव-व्यक्तित्व का समग्र विकास, मानव-स्वाधीनता की रक्षा, मुक्त-चिंतन का विकास है। |
| उपसंहार |